भगवान् के जन्म की तरह उस कर्म का भी, जिसके लिये अवतार हुआ करता है द्विविध भाव और द्विविध रूप होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया के जिस विधान के द्वारा, उत्थान और पतनरूपी जिस सहज व्यवस्था के द्वारा प्रकृति अग्रसर होती है, उस विधान और व्यवस्था के होते हुए भागवत धर्म की रक्षा और पुनर्गठन के लिये इस बाह्य जगत् पर भागवत शक्ति की जो क्रिया होती है, वही दिव्य कर्म का बाह्म पहलू है, और यह भागवत धर्म की मानवजाति के भगवन्मुख प्रयास को समस्त विघ्न-बाधाओं से उबारकर निश्चित रूप से आगे बढ़ाता है इसका आंतर पहलू यह है कि भवन्मुख चैतन्य की दिव्य शक्ति व्यक्ति और जाति की आत्मा पर क्रिया करती है ताकि वह मानवरूप में अवतरिक भगवान् के नये-नये प्रकाश को ग्रहण कर सके और अपने ऊर्ध्वमुखी आत्म-विकास की शक्ति को बनाये रख सके, उसमें एक नवजीवन ला सके और उसे समृद्ध कर सके। अवतार का अतरण केवल किसी महान् बाह्य कर्म के लिये नहीं होता जैसा कि मनुष्य की कर्म-प्रवण बुद्धि समझा करती है। कर्म और बाह्म घटना का अपने-आपको कोई मूल्य नहीं होता, उनका मूल्य उस शक्ति पर आश्रित है जिनकी ओर से वे होते हैं और उस भाव पर आश्रित हैं जिसके वे प्रतीक होते हैं और जिसे सिद्ध करना ही उस शक्ति का काम होता है।
जिस संकट की अवस्था में अवतार का आभिभार्व होता है वह बाहरी नजर को महज घटनाओं और जड़ जगत् के महत् परिवर्तनों का नाजुक काल प्रतीत होता है। परंतु उसे स्त्रोत और वास्तविक अर्थ को देखें तो यह संकट मानव-चेतना में तब आता है जब उसका कोई महान परिवर्तन, कोई नवीन विकास होने वाला हो। इस परिवर्तन के लिये किसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता होती है, किंतु शक्ति जिस चेतना में काम करती है उसके बल के अनुसार बदलती है; इसलिये मानव-मन और अंतरात्मा में भागवत चैतन्य का अविर्भाव आवश्यक होता है। जहाँ मुख्यतः बौद्धिक और लौकिक परिवर्तन करना हो वहीं अवतार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती; मानव-चेतना का उत्थान होता है, शक्ति की महान अभिव्यक्ति होती है जिसके फलस्वरूप सामयिक तौर पर मनुष्य अपनी साधारण अवस्था से ऊपर उठ जाते हैं और चेतना और शक्ति की यह लहर कुछ असाधारण व्यक्त्यिों में तरंग-श्रंग बन जाती है और इन्हीं असाधारण व्यक्तियों को विभूति कहते हैं; इन विभूतियों का काम सर्वसाधारण मानवजाति के कर्म का नैतृत्व करना है और यह उद्दिष्ट परिवर्तन के लिये पर्याप्त होता है। यूरोपीय पुनर्निर्माण और फ्रांस की राज्य-क्रांति इसी प्रकार के संकट थे; महान् आध्यात्मिक घटनाएं, बल्कि बौद्धिक और लौकिक परिवर्तन थे। एक में धार्मिक तथा दूसरे में सामाजिक और राजनीतिक भावनाओं, रूपों और प्रेरकभावों का परिवर्तन हुआ और इसके फलस्वरूप जनसाधारण की चेतना में जो फेरफार हुआ वह बौद्धिक और लौकिक था, आध्यात्मिक नहीं।
पर जब किसी संकट के मूल में कोई आध्यात्मिक बीज या हेतु होता है तब मानव-मन और आत्मा में प्रवर्तक और नेता के रूप से भागवत चैतन्य का पूर्ण या आंशिक प्रादुर्भाव होता है। यही अवतार है। अवतार के बाह्य कर्म का वर्णन गीता में धर्मसंस्थापनार्थाय कहकर किया गया है; जब-जब धर्म की ग्लानि या हृास होता है, उसका बल क्षीण हो जाता है और अधर्म सिर उठाता, प्रबल होता और अत्याचार करता है तब-तब अवतर आते और धर्म को फिर से शक्तिशाली बनाते हैं। जो बातें विचार के अंतर्गत होती हैं वे कर्म के द्वारा तथा विचारों की प्रेरणा का अनुगमन करने वाले मानव-प्राणी के द्वारा प्रकट होती है, इसलिये अत्यंत मानवी और लौकिका भाषा में अवतार का काम है प्रतिगामी अंधकार के राज्य द्वारा सताये गये धर्म के अन्वेशषकों की रक्षा करना, और अधर्म को बनाये रखने की इच्छा करने वाले दुष्टों का नाश करना। परंतु इस बात को कहने में गीता ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनकी ऐसी संकीर्ण और अधूरी व्याख्या की जा सकती है।जिससे अवतार का आध्यात्मिक गंभीर अर्थ जाता रहे। धर्म एक एक ऐसा शब्द है जिसका नैतिक और व्यावहारिक, प्राकृतिक और दार्शनिक, धार्मिक और आध्यात्कि, सभी प्रकार का अर्थ होता है और इनमें से किसी भी अर्थ में इस शब्द का इस तरह से प्रयोग किया जा सकता है कि उसमें अन्य अर्थों की गुजांयश न रहे, उदाहरणार्थ, इसका केवल नैतिक अथवा केवल दार्शनिक या केवल धार्मिक अर्थ किया जा सकता है।
नैकित रूप से सदाचार के नियम को, जीवनचर्या-संबंधी नैतिक विधान को अथवा और भी बाह्म और व्यावहारिक अर्थ मगर सामाजिक और राजनीतिक न्याय को या केवल सामाजिक नियमों के पालन को धर्म कहा जाता है। यदि हम इस शब्द को इसी अर्थ में ग्रहण करें, तो इसका यही अभिप्राय हुआ कि जब अनाचार, अन्याय और दुराचार का प्राबल्य होता है तब भगवान् अवतार लेकर सदाचारियों को बचाते और दुराचारियों को नष्ट करते हैं, अन्याय और अत्याचार को रौंद डालते और न्याय और सद्व्यवहार को स्थापित करते हैं ।कृष्णवतार का प्रसिद्ध पौराणिक वर्णन इसी प्रकार का है। कौरवों का अत्याचार, दुर्योधनादि जिसके मूर्त रूप हैं, इतना बढ़ा कि पृथ्वी के लिये उसका भार असह्य हो उठा और पृथ्वी को भगवान् से अवतार लेने और भार हल्का करने की प्रार्थना करनी पड़ी, तदानुसार विष्णु श्री कृष्णरूप में अवतीर्ण हुए, उन्होंने अत्याचार-पीड़ित पांडवों का उद्धार और अन्यायी कौरवों का संहार किया। उसके पूर्व अन्यायी अत्याचारी रावण का वध करने के लिये जो विष्णु का रामावतार अथवा क्षत्रियों की उद्दंडता को नष्ट करने के लिये परशुरामवतार या दैत्याज बलि के राज्य को मिटाने के लिये वामनावतार हुआ उसका भी ऐसा ही वर्णन है। परंतु यह प्रत्यक्ष है कि पुराणों के इस प्रसिद्ध वर्णन से कि अवतार इस प्रकार के सर्वथा व्यावहारिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्म को करने के लिये आते हैं, अवतार के कार्य का सच्चा विवरण नहीं मिलता।
इस वर्णन में अवतार के आने का आध्यात्मिक हेतु छूट जाता है; और यदि इस बाह्य प्रयोजन को ही हम सब कुछ मान लें तो बुद्ध और ईसा को हमें अवतारों की कक्षा से अलग कर देना होगा, क्योंकि इनका काम तो दुष्टों को नष्ट करने और शिष्टों को बचाने का नहीं, बल्कि अखिल मानव-समाज को एक नया आध्यात्मिक संदेश सुनाना तथा दिव्य विकास और आध्यात्मिक सिद्धि का एक नया विधान देना था। धर्म शब्द को यदि हम केवल धार्मिक अर्थ में ही ग्रहण करें अर्थात् इसे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का एक विधान मानें तो हम इस विषय के मूल में तो जरूर पहूंचेगे, किंतु इसमें भय है कि हम अवतार के एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य को कहीं दृष्टि की औट न कर दे। भगवद्वतारों के इतिहास में सर्वत्र ही यह स्पष्ट दिखायी देता है कि उनका कार्य द्विविध होता है और यह अपरिहार्य है, द्विविध होने का कारण यह है कि अवतीर्ण भगवान् मानव-जीवन में होने वाले भगवत-कार्य को ही अपने हाथ में उठा लेते हैं, जगत् में जो भगवत-इच्छा और भगवत-ज्ञान काम कर रहे हैं, उन्हीं का अनुसरण कर अपना कार्य करते हैं और यह कार्य सदा आंतर और बाह्म दोनों प्रकार से सिद्ध होता है-आत्मा में आंतरिक उन्नति के द्वारा और जागतिक जीवन में बाह्म परिवर्तन द्वारा हो सकता है कि भगवान् का अवतार, किसी महान् आध्यात्मिक गुरु या त्राता के रूप में हो,
जैसे बुद्ध और ईसा, किंतु सदा ही उनकी पार्थिव अभिव्यक्ति की समाप्ति के बाद भी उनके कर्म के फलस्वरूप जाति के केवल नैतिक जीवन में ही नहीं बल्कि उसके सामाजिक और बाह्म जीवन और आदर्शों में भी एक गंभीर और शक्तिशाली परिवर्तन हो जाता है। दूसरी ओर, हो सकता है कि वे दिव्य जीवन, दिव्य व्यक्तित्व और दिव्य शक्ति के अवतार होकर आवें, अपने दिव्य कर्म को करने के लिये, जिसका उद्देश्य बाहर से सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक ही दिखयी देता हो; जैसा कि राम और कृष्ण की कथाओं में बताया गया है, फिर भी सदा ही यह अवतरण जाति की आत्मा में उसके आंतरिक जीवन के लिये और उसके आध्यात्मिक नव जन्म के लिये एक ऐसी स्थायी शक्ति का काम करता है। यह एक अनोखी बात है कि बौद्ध और इसाई धर्मों का स्थायी, जीवंत तथा विश्वव्यापक फल यह हुआ कि जिन मनुष्यों तथा कालों ने इनके धार्मिक और आध्यात्मिक मतों, रूपों और साधनाओं का परित्याग कर दिया, उन पर भी इन धर्मों के नैतिक, सामाजिक और वयावहारिक आदर्शो का शक्तिशाली प्रभाव पड़ा। पीछे के हिन्दुओं ने बुद्ध, उनके संघ और धर्म को अमान्य कर दिया, पर बुद्धधर्म के सामाजिक और नैतिक प्रभाव की अमिट छाप उन पर पड़ी हुई है और हिंदूजाति का जीवन और आचार-विचार उससे प्रभावित है।
आधुनिक यूरोप नाममात्र का ईसाई है, पर इसमें जो मानवदया का भाव है वह ईसाई-धर्म के आध्यात्मिक सत्य का सामाजिक और राजनीतिक रूपांतर है; और स्वाधीनता, समता और विश्वबंधुता की यह अभीप्सा मुख्यतः उन लोगों ने की जिन्होंने ईसाई-धर्म और आध्यात्मिक साधना को व्यर्थ तथा हानिकर बतलाकर त्याग दिया था और यह काम उस युग में हुआ जिसने स्वतंत्रता के बौद्धिक प्रयास में ईसाई-धर्म को धर्म मानना छोड़ देने की पूरी कोशिश की। राम और कृष्ण की जीवनलीला ऐतिहासिक काल के पूर्व की है, काव्य और आख्यायिका के रूप में हमें प्राप्त हुई है और इसे हम चाहें तो केवल काल्पनिक कहानी भी कह सकते हैं; पर चाहे काल्पनिक कहानी कहिये या ऐतिहासिक तथ्य, इसका कुछ महत्त्व नहीं; क्योंकि उनके चरित्रों का जो शाश्वत सत्य और महत्त्व है वह तो इस बात में है कि ये चरित्र जाति की आंतरिक चेतना और मानव-जीव के जीवन में सदा के लिये एक आध्यात्मिक रूप, सत्ता और प्रभाव के रूप में अमर हो गये हैं। अवतार दिव्य जीवन और चैतन्य के तथ्य हैं; वे किसी बाह्य कर्म में भी उतर सकते हैं, पर उस कर्म के हो चुकने और उनका कार्य पूर्ण होने के बाद भी उस कर्म का आध्यात्मिक प्रभाव बना रहता है; अथवा वे किसी आध्यात्मिक प्रभाव को प्रकटाने और किसी धार्मिक शिक्षा को देने के लिये भी प्रकट हो सकते हैं, किंतु उस हालत में भी, उस नये धर्म या साधना के क्षीण हो चुकने पर भी, मानवजाति के विचार, उसकी मनोवृत्ति और उसके बाह्य जीवन पर उनका स्थायी प्रभाव बना रहता है। इसलिये अवतार-कार्य के गीतोक्त वर्णन को ठीक तरह से समझाने के लिये आवश्यक है कि हम धर्म शब्द के अत्यंत पूर्ण, अत्यंत गंभीर और अत्यंत व्यापक अर्थ को ग्रहण करें, धर्म को वह आंतर और बाह्य विधान समझें जिसके द्वारा भागवत संकल्प और भागवत ज्ञान मानवजाति का आध्यात्मिक विकास साधन करते हैं और जाति के जीवन में उसके विशिष्ट परिस्थितियां और उनके परिणाम निर्मित करते हैं। भारतीय धारणा के हिसाब से धर्म केवल शुभ, उचित, सदाचार, न्याय और आचारनीति ही नहीं बल्कि अन्य प्राणियों के साथ, प्रकृति और ईश्वर के साथ मनुष्यों के जितने भी संबंध हैं उन सबका संपूर्ण नियमन है और यह नियामक तत्त्व ही वह दिव्य धर्मतत्त्व है जो जगत् के सब रूपों और कर्मों के द्वारा, आंतर और बाह्य जीवन के विविध आकारों के द्वारा तथा जगत् में जितने प्रकार के परस्पर-संबंध हैं उनकी व्यवस्था के द्वारा अपने-आपको सिद्ध करता रहता है। धर्म वह है जिसे हम धारण करते हैं और वह भी जो हमारी सब आंतर और बाह्य क्रियाओं को एक साथ धारण किये रहता है। धर्म शब्द का प्राथमिक अर्थ हमारी प्रकृति का वह मूल विधान है जो गुप्त रूप से हमारे कर्मों को नियत करता है और इसलिये इस दृष्टि से प्रत्येक जीव, प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक जाति, प्रत्येक व्यक्ति और समूह का अपना-अपना विशिष्ट धर्म होता है।
दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर जो भागवत प्रकृति है उसे भी तो हमारे अंदर विकसित और व्यक्त होना है, और इस दृष्टि से धर्म अंतः-क्रियाओं का वह विधान है जिसके द्वारा भागवत प्रकृति हमारी सत्ता में विकसित होती है। फिर एक तीसरी दृष्टि से धर्म वह विधान है जिससे हम अपने बहिर्मुखी विचार, कर्म और पारस्परिक संबंधो का नियंत्रण करते हैं ताकि भागवत आदर्श की ओर उन्नत होने में हमारी और मानवजति की अधिक-से-अधिक सहायता हो। धर्म को साधारणतया सनातन और अपरिवर्तनीय कहा जाता है, और इसका मूल तत्त्व और आदर्श हो भी ऐसा ही; पर इसके रूप निरंतर बदला करते हैं, उनका विकास होता रहता है; कारण मनुष्य अभी उस आदर्श को प्राप्त नहीं किया है या यह कहिये कि उसमें अभी उसकी स्थिति नहीं है; अभी तो इतना ही है कि मनुष्य उसे प्राप्त करने की अधूरी या पूरी इच्छा कर रहा है, उसके ज्ञान और अभ्यास की ओर आगे बढ़ रहा है। और इस विकास में धर्म वही है जिससे भागवत पवित्रता, विशालता, ज्योति, स्वतंत्रता, शक्ति, बल, आनंद, प्रेम, शुभ, एकता, सौन्दर्य हमें अधिकाधिक प्राप्त हों।
इसके विरुद्ध इसकी परछाई और इनकार खड़ा है, अर्थात् वह सब जो इसकी बुद्धि का विरोध करता है, जो इसके विधान के अनुगत नहीं है, वह जो भागवत संपदा के रहस्य को न तो समर्पण कारण है न समर्पण करने की इच्छा रखता है, बल्कि जिन बातों को मनुष्य को अपनी प्रगति के मार्ग में पीछे छोड़ देना चाहिये, जैसे अशुचिता, संकीर्णता, बंधन, अंधकार, दुर्बलता, नीचता, असामंजस्य, दुःख, पार्थक्य, वीभत्सत्ता और असंस्कृति आदि एक शब्द में, जो कुछ धर्मों का विकार और प्रत्याख्यान है उस सबका मोरचा बनाकर सामने डट जाता है यही अधर्म है जो धर्म से लड़ता और उसे जीतना चाहता है, जो उसे पीछे और नीचे की ओर खींचना चाहता है, यह वह प्रतिगामी शक्ति है जो अशुभ, अज्ञान और अंधकार का रास्ता साफ करती है। इन दोनों में सतत संग्राम और संर्घष चल रहा है, कभी इस पक्ष की विजय होती है कभी उस पक्ष की, कभी ऊपर की ओर ले जाने वाली शक्तियों की जीत होती है तो कभी नीचे की ओर खींचने वाली शक्तियों की। मानव-जीवन और मानव-आत्मा पर अधिकार जमाने के लिये जो संग्राम होता है उसे वेदों ने देवासुर-संग्राम कहा है (देवता अर्थात् प्रकाश और अखंड अनंतता के पुत्र, असुर अर्थात् अंधकार और भेद की संतान); जरथुस्त्र के मत में यही अहुर्मज्द-अहिर्मन-संग्राम है और पीछे के धर्मसंप्रदायों में इसीको मानव जीवन और आत्मा पर अधिकार करने के लिये ईश्वर और उनके फरिश्तों के साथ शैतान या इबलीस और उनके दानवों का संग्राम कहा गया है।
यही बात अवतार के कर्म का स्वरूप निश्चित और निर्धारित करती है। बौद्धमताव-लंबी साधक अपनी मुक्ति के विरोधी तत्त्वों से बचने के लिये धर्म, संघ और बद्ध, इन तीन शक्तियों की शरण लेते हैं। ईसाई मत में भी ईसाई जीवनचर्या, गिरिजाघर और स्वयं ईसा है। अवतार के कार्य में ये तीन बातें अवश्य होती हैं। अवतार एक धर्म बतलाते हैं, आत्मा-अनुशासन का एक विधान बतलाते हैं, जिससे मनुष्य निम्नतर जीवन से निकलकर उच्चतर जीवन में संवर्द्धित हों। धर्म में, सदा ही, कर्म के विषय में तथा दूसरे मनुष्य और प्राणियों के साथ साधक का क्या संबंध होना चाहिये इस विषय में एक विधान भी रहता है, जैसे कि अष्टांग-मार्ग अथवा श्रद्धा, प्रेम और पवित्रता का धर्म अथवा इसी प्रकार का और कोई धर्म जो अवतार के भागवत स्वभाव में प्रकट हुआ हो। इसके बाद, चूंकि मनुष्य की प्रवृत्ति के सामूहिक और वैयक्तिक पहलू होते हैं, जो लोग एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं उनमें स्वभावतः एक आध्यात्मिक साहचर्य एकता स्थापित हो जाती है, इसलिये अवतार एक संघ की स्थापना करते हैं, संघ अर्थात् उन लोगों का सख्य और एकत्व जो अवतार के व्यक्तित्व और शिक्षा के कारण एक सूत्र में बध जाते हैं। यही त्रिक ‘‘भागवत, भक्त और भगवान्” के रूप से वैष्णव धर्म में भी है।
वैष्णव-धर्मसम्मत उपासना और प्रेम का धर्म ही भागवत है, उस धर्म का जिन लोगों में प्रादुर्भाव होता है उन्हीं का संघ-समुदाय भक्त कहता है, और जिन प्रेमी और प्रेमास्पद की सत्ता और स्वभाव में यह प्रेममय भागवत धर्म प्रतिष्ठित है और जिनमें इसकी पूर्णता होती है वही भगवान् हैं। अवतार त्रिक के इस तृतीय तत्त्व के प्रतीक हैं, वह भागवत व्यक्त्त्वि, स्वभाव और सत्ता हैं जो इस धर्म और संघ की आत्मा हैं, और वे इस धर्म और संघ को अपने द्वारा अनुप्राणित करते हैं, उसे सजीव बनाये रखते हैं तथा मनुष्यों को आनंद और मुक्ति की ओर आकर्षित करते हैं। गीता की शिक्षा में, जो अन्य विशिष्ट शिक्षाओं और साधनाओं की अपेक्षा अधिक उदार और बहुमुखी है, ये तीन बातें भी बहुत व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यहाँ की एकता सबको अपने साथ मिला लेने वाली वह वैदांतिक एकता है जिसके द्वारा जीव सबको अपने अंदर और अपने-आपको सबके अंदर देखता और सब प्राणियों के साथ अपने-आपको एक कर लेता है। इसलिये सब मानव संबंधों को उच्चतर दिव्य अभिप्राय में ऊपर उठाना ही धर्म है। यह धर्म भगवान् की खोज करने वाला साधक जिस समाज में रहता है, उस समग्र मानव-समाज को एक सूत्र में बांधने वाले नैतिक, सामाजिक और धार्मिक विधान से आरम्भ होता है और उसे ब्राह्यी चेतना द्वारा अनुप्राणित करके ऊपर उठा देता है; वह एकता, समता और मुक्त निष्काम भगवत्परि-चालित कर्म का विधान देता है, ईश्वर-ज्ञान और आत्म-ज्ञान का वह विधान देता है जो समस्त प्रकृति और समस्त कर्म को अपनी ओर खींचता और आलोकित करता है।
मानव-समाज को भागवत सत्ता और भागवत चेतना की ओर आकर्षित करता है, तथा भागवत प्रेम का वह विधान देता है जो ज्ञान और कर्म की शक्ति है, चरम सिद्धि है। गीता में जहाँ प्रेम और भक्ति के द्वारा भगवन् को पाने की साधना बतलायी गयी है वहीं संघ और भागवत भक्तों के द्वारा भगवत्प्रेम और भगवदनुसंधान में सख्य और परस्पर-साहाय्य का मौलिक भाव आ गया है, पर गीता की शिक्षा का असली संघ तो समग्र मानवजाति है सारा जगत् और अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक मुनष्य इसी धर्म की ओर जा रहा है। ‘‘यह मेरा ही तो मार्ग है जिसपर सब मनुष्य चले आ रहे हैं, ” और वह भवदन्वेषक जो सबके साथ एक हो जाता, सबके सुख-दुःख तथा समस्त जीवन को अपना सुख दुःख और जीवन बना लेता है, वह मुक्त पुरुष जो सब भूतों के साथ एकात्मभाव को प्राप्त हो चुका है, वह समर्ग मानवजाति के जीवन में ही वास करता है, मावजाति के अखिलांतरात्मा के लिये, सर्वभूतांतरात्मा भगवान् के लिये ही जीता है, वह लोक-संग्रह के लिये अर्थात् सबमें अपने-आपको विशिष्ट धर्म में और सार्वभौम धर्म में स्थित रखने के लिये, उन्हें सब अवस्थाओं और सब मार्गों से भगवान् की ओर ले जाने के लिये कर्म करता है।
क्योंकि यद्यपि स्थल पर अवतार श्रीकृष्ण ने नाम और स्पष्ट में प्रकट हैं पर वे अपने मानवजन्म के इस एक रूप पर ही जोर नहीं दे रहे; बल्कि उन भगवान पुरुषोत्तम की बात कह रहे हैं जिनका यह एक रूप है, समस्त अवतार जिनके मानवजन्म हैं और मनुष्य जिन-जिन देवताओं के नाम और उनकी पूजा करते हैं, वे सब भी उन्हीं के रूप हैं। श्रीकृष्ण ने जिस मार्ग का वर्णन किया है उसके बारे में यद्यपि यह घोषित किया गया है कि यह वह मार्ग है जिसपर चलकर मुनष्य सच्चे ज्ञान और सच्ची मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, किंतु यह वह मार्ग है जिसमें अन्य सब मार्ग समाये हुए हैं, उनका इसमें बहिष्कार नहीं है। भगवान् अपनी विश्वव्यापकता में समस्त अवतारों, समस्त शिक्षाओं और समस्त धर्मों को लिये हुए है। यह जगत् जिस युद्ध की रंगभूमि है गीता उसके दो पहलूओं पर जोर देती है, एक आंतरिक संघर्ष, दूसरा बाह्म युद्ध। आंतरिक संघर्ष में शत्रुओं का दल अंदर, व्यक्ति के अपने अंदर है, और इसमें कामना, अज्ञान और अंकार को मारना ही विजय है। पर मानव-समूह के अंदर धर्म और अधर्म की शक्त्यिों के बीच एक बाह्म युद्ध भी चल रहा है। भगवान्, मनुष्य की देवोपम प्रकृति और उसे मानवजीवन में सिद्ध करने का प्रयास करने वाली शक्तियां धर्म की सहायता करती हैं। उद्दंड अहंकार ही जिनका अग्रभाग है ऐसी आसुरी या राक्षसी प्रकृति, अहंकार के प्रतिनिधि और उसे संतुष्ट करने का प्रसास करने वालों को साथ लेकर अधर्म की सहायता करती है।
यही देवासुरसंग्राम है जो प्रतीक-रूप से प्राचीन भारतीय साहित्य में भरा है। महाभारत के महायुद्ध को, जिसमें मुख्य सूत्रधार श्रीकृष्ण हैं, प्रायः इसी देवासुर-संग्राम का एक रूपक कहा जाता है; पाण्डव, जो धर्मराज्य की स्थापना के लिये लड़ रहे हैं, देवपुत्र हैं, मानव रूप में देवताओं की शक्तियां हैं और उनके शत्रु आसुरी शक्ति के अवतार हैं, असुर हैं, इस बाह्य संग्राम भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करने, असुरों अर्थात् दुष्टों का राज्य नष्ट करने, उन्हें चलाने वाली आसुरी शक्ति का दमन करने और धर्म के पीड़ित आदर्शों को पुनः स्थापित करने के लिये भगवान् अवतार लिया करते हैं। व्यष्टिगत मानव-पुरुष में स्वर्गराज्य का निर्माण करना जैसे भगवदवतार का उद्देश्य होता है वैसे ही मानव-समष्टि के लिये भी स्वर्गराज्य को पृथ्वी के निकटतर ले आना उनका उद्देश्य होता है। भगवदावतार के आने का आंतरिक फल उन लोंगों को प्राप्त होता है जो भगवान् की इस क्रिया से दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के वास्तविक मर्म को जान लेते और अपनी चेतना में भगवन्मय होकर, सर्वथा भगवदाश्रित होकर रहते, और अपने ज्ञान की तपः शक्ति से पूत होकर, अपा प्रकृति से मुक्त होकर भगवान् के स्पस्ट और स्वभाव को प्राप्त होते हैं मनुष्य के अंदर इस अपरा प्रकृति के ऊपर जो दिव्य प्रकृति है उसे प्रकटाने के लिये तथा बंधरहित, निरंहकार, निष्काम, नैवर्यक्तिक, विश्वव्यापक, भागवत ज्योति, शक्ति और प्रेम से परिपूर्ण दिव्य कर्म दिखने के लिये भगवान् का अवतार हुआ करता है। भगवन् आते हैं दिव्य व्यक्तित्व के रूप में, वह व्यक्तित्व जो मनुष्य की चेतना में बस जायेगा और उसके अहंभावापन्न परिसीमित व्यक्तित्व की जगह ले लेगा जिससे कि मनुष्य अहंकार से मुक्त होकर अनंता और विश्वव्यापकता में फैल जाये, जन्म के पचड़े से निकलकर अमर हो जाये। भगवान् भागवत शक्ति और प्रेम के रूप में आते हैं जो मनुष्यों को अपनी ओर बुलातें हैं ताकि मुनष्य उन्हीं का आश्रय लें और अपने मानव संकल्पों को त्याग दें, अपने काम-क्रोध और भयजनित द्वंद्वों से छूट जायें और इस महान् दुःख और अशांति से मुक्त होकर भागवत शांति और आनंद में निवास करे। जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं यो वेत्ति तत्त्वत: । त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥4.9॥ वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता: । बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता: ॥4.10॥ अवतार किसी रूप में, किस नाम से आवेंगे और भगवान् के पहलू को सामने रखेंगे, इसका विशेष महत्त्व नही है; क्योंकि मनुष्यों की भिन्न-भिन्न प्रकृति के अनुसार जितने भी विभिन्न मार्ग हैं उन सभी में मनुष्य भगवान् के द्वारा अपने लिये नियत मार्ग पर चल रहे हैं जो अंत में उन्हें भगवान् के समीप ले जायेगा। भगवान् का वही पहलू मनुष्यों की प्रकृति के अनुकूल होता है जिसका वे उस समय अच्छी तरह से अनुसरण करें जब भगवान् नेतृत्व करने आये, मनुष्य चाहे जिस तरह भगवान् को अपनायें उनसे प्रेम करें और आनंदित हों, भगवान् उन्हें उसी तरह से अपनाते, उनसे प्रेम करते और आनंदित होते हैं, ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहम्।
दिव्य जन्म को प्राप्त होना-अर्थात् जीव का किसी उच्चतर चेतना में उठकर दिव्य अवस्था को प्राप्त कराने वाले नवजन्म को प्राप्त होना-और दिव्य कर्म करना, सिद्धि से पहले साधन के तौर पर और पीछे उस दिव्य जन्म की अभिव्यक्ति के तौर पर, यही गीता का संपूर्ण कर्मयोग है। गीता दिव्य कर्म के ऐसे बाह्य लक्षण नहीं बतलाती जिनसे बाह्य दृष्टि से उसकी पहचान की जा सके या लौकिक आलोचना-दृष्टि से उसकी जांच की जा सके; सामान्य नीति धर्म के जो लक्षण हैं जिनसे मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार कर्तव्याकर्तव्य निश्चित करते हैं उन लक्षणों को भी गीता ने जान-बूझकर त्याग दिया है। गीता जिन लक्षणों से दिव्य कर्म की पहचान कराती है वे अत्यंत निगूढ़ और अंत:स्थ हैं; जिस मुहर से दिव्य कर्म पहचाने जाते हैं वह अलक्ष्य, आध्यात्मिक और नीतिधर्म से परे है। दिव्य कर्म आत्मा से उद्भूत होते हैं और केवल आत्मा के प्रकाश से ही पहचाने जा सकते हैं। ‘‘बड़े-बड़े ज्ञानी भी, ‘कर्म क्या है और अकर्म क्या है”, इसका निश्चय करने में मोहताज हो जाते हैं ”क्योंकि व्यावहारिक, सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक मानदंड से वे इनके बाह्य लक्षणों को ही पहचान पाते हैं, इनकी जड़ तक नहीं पहुच पाते; ‘मैं तुझे वह कर्म बतलाऊंगा जिसे जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जायेगा।
कर्म क्या है इसको जानना होगा, विकर्म क्या है इसको भी जनाना होगा और अकर्म क्या है यह भी जान लेना होगा; कर्म की गति गहन है।” [1] संसार में कर्म जंगल-सा है, जिसमें मनुष्य अपने काल की विचारधारा, अपने व्यक्तित्व के मानदंड और अपनी परिस्थिति के अनुसार लुढ़कता-पुढ़कता चलता है; और ये विचार और मान शासक एक ही काल या एक ही व्यक्तित्व को नहीं, बल्कि अनेक कालों और व्यक्तित्वों को लिये हुए होते हैं, अनेक सामाजिक अवस्थाओं के विचार और नीति-धर्म तह-पर-तह जमकर आपस में बंधे होते और यद्यपि इनका दावा होता है कि ये निरपेक्ष ओर अविनाशी हैं फिर भी तात्कालिक और रूढ़िगत ही होते हैं, यद्यपि ये अपने को सद्युक्ति की तरह दिखाने का ढोंग करते हैं पर होते अशास्त्रीय और अयौक्तिक ही। इस सबके बीच सुनिश्चित कर्म-विधान के किसी महत्त्म आधार और मूल सत्य को ढूंढ़ता हुआ ज्ञानी अंत में ऐसी जगह जा पहुँचता है जहाँ यही अंतिम प्रश्न उसके सामने आता है कि यह सारा कर्म और जीवन केवल एक भ्रमजाल तो नहीं है और कर्म को सर्वथा परित्याग कर अकर्म को प्राप्त होना ही क्या इस थके हुए, भ्रांतियुक्त मानवजीव के लिये अंतिम आश्रय नहीं है। परंतु श्रीकृष्ण कहते हैं कि इस बारे में ज्ञानी भी भ्रम में पड़ते और मोहित हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञान और मोक्ष कर्म से मिलते हैं, अकर्म से नहीं।
तब हल क्या है? वह किसी प्रकार का कर्म है जिससे हम जीवन के अशुभ से छूट सकें, इस संशय, प्रमाद और शोक से, अने विशुद्ध अद्हेतु-प्रेरित कर्मों के भी अच्छे-बुरे, अशुद्ध और भरमाने वाले परिणाम से, इन सहस्रों प्रकार की बुराइयों और दुःखो से, मुक्त हो सकें? उत्तर मिलता है कि कोई बाह्य प्रभेद करने की आवश्यकता नहीं; संसार में जो कर्म आवश्यक हैं उनसे बचने की आवश्यकता नहीं; हमारी मानव-कर्मण्यताओं की हदबन्दी की जरूरत नहीं, बल्कि सब कर्म किये जायें अंतरात्मा को भगवान् के साथ योग में स्थित करके, अकर्म मुक्ति का मार्ग नहीं है; जिसकी उच्चतम बुद्धि की अंतर्दृष्टि खुल गयी है वह देख सकता है कि इस प्रकार का अकर्म स्वयं ही सतत होने वाला एक कर्म है, एक ऐसी अवस्था है जो प्रकृति और उसके गुणों की क्रियाओं के अधीन है। शारीरिक अकर्मण्यता की शरण लेने वाला मन अभी इसी भ्रम में पड़ा है कि वह स्वयं कर्मों का कर्ता है, प्रकृति नहीं; उसने जढ़ता को मोक्ष समझ लिया होता, वह यह नहीं देख पाता कि जो ईंट-पत्थर से भी अधिक जढ़ दिखाई देता है उसमें भी प्रकृति की क्रिया हो रही होती है, उस पर भी प्रकृति अपना अधिकार अक्षुण्ण रखती है। इसके विपरीत, कर्म के पूर्ण प्लावन में भी आत्मा अपने कर्मों से मुक्त है, वह कर्ता नहीं है जो कुछ किया जा रहा है उससे बद्ध नहीं है।
जो आत्मा की इस मुक्तावस्था में रहता है और प्रकृति के गुणों में बंधा नहीं है, वही कर्मों से मुक्त रहता है। गीता के इस वाक्य का कि ‘‘जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वही मनुष्यों में विवेकी और बुद्धिमान् है, ”स्पष्ट रूप से यही अभिप्राय है। गीता का यह वाक्य सांख्य ने पुरुष और प्रकृति के बीच जो भेद किया है उस पर प्रतिष्ठित है-वह भेद यह है कि पुरुष नित्य मुक्त, अकर्ता, चिरशांत, शुद्ध तथा कर्मों के अंदर भी अविचल है और प्रकृति चिरक्रियाशीला है जो जढ़ता और अकर्म की अवस्था में भी उतनी ही कर्मरत है जितनी कि दृश्य कर्मस्त्रोत के कोलाहल में। यही वह उच्चतम ज्ञान है जो बुद्धि के उच्चतम प्रयास से प्राप्त होता है, इसलिये जिसने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है वही यथार्थ में बुद्धिमान् है, वह भ्रांत मोहित बुद्धिवाला मनुष्य नहीं जो जीवन और कर्म को निम्नतार बुद्धि के बाह्य, अनिश्चित और अस्थायी लक्षणों से समझना चाहता है। इसलिये मुक्त पुरुष कर्म से भीत नहीं होता, वह संपूर्ण कर्मों का करने वाला विशाल विराट कर्मी होता है, वह औरों की तरह प्रकृति के वश में रहकर कर्म नहीं करता है, वह आत्मा की नीरव स्थिरता में प्रतिष्ठित होकर, भगवान् के साथ योगयुक्त होकर कर्म करता है। उसके कर्मों के स्वामी भगवान् होते हैं, वह उन कर्मों का निमित्तमात्र होता है जो उसकी प्रकृति अपने स्वामी को जानते हुए, उन्हीं के वश में रहते हुए करती है।
इस ज्ञान की धधकती हुई प्रबलता और पवित्रता में उसके कर्म अग्नि में ईधन की तरह जलकर भस्म हो जाते हैं और इनका उसे मन पर कोई लेप या दाग नहीं लगता, वह स्थिर, शांत, अचल, निर्मल, शुभ और पवित्र बना रहता है। कर्तृव्य-अभिमान से शून्य इस मोक्षदायक ज्ञान में स्थित होकर, समस्त कर्मों को करना ही दिव्य कर्मी का प्रथम लक्षण है। दूसरा लक्षण है कामना से मुक्ति; क्योंकि जहाँ कर्ता का व्यक्तिगत अहंकार नहीं होता वहाँ कामना का रहना असम्भव हो जाता है, वहाँ कामना निरहार हो जाती है, निराश्रय हो जाने के कारण अवसन्न होकर क्षीण और नष्ट हो जती है। बाह्मतः मुक्त पुरुष भी दूसरे लोगों की तरह ही समस्त कर्मों को करता हुआ दिखायी देता है शायद वह कर्मों को बड़े पैमाने पर और अधिक शक्तिशाली संकल्प और वेगवती शक्ति के साथ करता है, क्योंकि उसकी सक्रिय प्रकृति में भगवान् के संकल्प का बल काम करता है; परंतु उसके समस्त उपक्रमों और उद्योगों में कामना के हीनतर भाव और निम्नतर इच्छा का अभाव होता है, उनको अपने कार्मों के फल के लिये आसक्ति नहीं हेाती, और जहाँ फल के लिये कर्म नहीं किया जाता है बल्कि सब कर्मों के स्वामी का नैर्व्यक्तिक यंत्र बनकर ही सारा कर्म किया जाता है। वहाँ कामना-वासना के लिये कोई स्थान ही नहीं होता-वहाँ मालिक के काम को सफलतापूर्वक करने की कोई इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि फल तो भगवान् का है उन्हीं के द्वारा विहित है, किसी व्यक्तिगत इच्छा या प्रयत्न के द्वारा नहीं, वहाँ यह इच्छा भी नहीं होती कि मालिक के काम को गौरव के साथ करूं या इस प्रकार करूं जिससे मालिक संतुष्ट हों, क्योंकि यथार्थ में कर्मी तो स्वयं भगवान् हैं, सारी महिमा उनकी शक्ति के उस रूप-विशेष की जिसके जिम्मे प्रकृति में उस कर्म का भर सौंपा गया है, न कि किसी परिच्छिन्न मानव-व्यक्तित्व की। मुक्त पुरुष का अंत:करण और अंतरात्मा कुछ भी नहीं करता, यद्यपि वह अपनी प्रकृति के अंदर से कर्म में नियुक्त तो होता है, पर कर्म करती है वह प्रकृति, वह कन्नीं शक्ति, वह चिन्मयी भगवती जो अंतर्यामी भगवान् के द्वारा नियंत्रित होती है। इसका यह मबलब नही कि कर्म पूर्ण कौशल के साथ, सफलता के साथ, उपयुक्त साधनों का ठीक-ठीक उपयोग करके न किया जाये। बल्कि, योगस्थ होकर शांति के साथ कर्म करने से कुशल कर्म करना जितना अधिक सुलभ होता है उतनी आशा और भय से अंधे होकर या लुड़कती-पुड़ीकती बुद्धि के निर्णयों द्वारा लंगड़े बने हुए कर्मों को, या फिर अधीर मानव-इच्छा की उत्सुकता पूर्ण घबराहट के साथ दौड़-धूप करके कर्म करने से नहीं होता।
गीता ने अन्यत्र कहा है, योग ही है कर्म का सच्चा कौशल। पर यह सब होता है नैर्व्यक्तिक भाव से एक महती विश्व-ज्योति और शक्ति के द्वारा जो व्यष्टि-पुरुष की प्रकृति में से अपना कर्म करती है। कर्मयोगी इस बात को जानता है कि उसे जो शक्ति दी गयी है वह भगवत्-निर्दिष्ट फल को प्राप्त करने के उपयुक्त होगी, उसे जो कर्म करना है वह कर्म के पीछे जो भागवत चिंता है उसके अनुकूल होगा और उसका संकल्प, उसकी गतिशक्ति और दिशा गुप्त रूप से भागवत प्रज्ञा के द्वारा नियंत्रित होती रहेंगी-अवश्य ही उसका संकल्प न तो इच्छा होगी न वासना, बल्कि वह सचेतन शक्ति का किसी ऐसे लक्ष्य की ओर नैर्व्यक्तिक प्रवाह होगा जो उसका अपना नहीं है। कर्म का फल वैसा भी हो सकता है जिसे सामान्य मनुष्य सफलता समझते हैं अथवा ऐसा भी हो सकता है जो उन्हें विफलता जान पड़े, पर कर्मयोगी इन दोनों में अभीष्ट की सिद्धि ही देखता है, और वह अभीष्ट उसका अपना नहीं, बल्कि उन सर्वज्ञ का होता है जो कर्म और फल, दोनों के संचालक हैं। कर्मयोगी विजय की खोज नहीं करता, वह तो यही इच्छा करता है कि भगवत्संकल्प और भगवदभिप्राय पूर्ण हो और यह पूर्णता आपातदृश्य पराजय के द्वारा भी उतनी ही साधित होती है जितनी जय के द्वारा और प्रायः जय की अपेक्षा पराजय के द्वारा यह कार्य विशेष बल के साथ संपन्न होता है।
अर्जुन को युद्ध के आदेश के साथ-साथ विजय का आश्वासन भी प्राप्त है; पर यदि उसकी हार होनी होती तो भी उसका कर्तव्य युद्ध ही होता; क्योंकि जिन क्रियाशक्तियों के समूह के द्वारा भगवान् का संकल्प सफल होता है उसमें तत्काल भाग लेने के लिये अर्जुन को उस समय यह युद्ध-कर्म सौंपा गया। मुक्त पुरुष की व्यक्त्गित आशा-आकांक्षा नहीं होती; वह चीजों को अपनी वैयक्त्कि संपत्ति जानकर पकड़े नहीं रहता; भगवत्सकंल्प जो ला देता है वह उसे ग्रहण करता है, वह किसी वस्तु का लोभ नहीं करता, किसी से डाह नहीं करता; जो कुछ प्राप्त होता है उसे वह राग-द्वेषरहित होकर ग्रहण करता है; जो कुछ चला जाता है उसे संसार-चक्र में जाने देता है और उसके लिये दुःख या शोक नहीं करता, उसे हानि नहीं मानता। उसका हृदय और आत्मा पूर्णतया उसके वश में होते हैं, वे समस्त प्रतिक्रिया या आवेश से मुक्त होता है, वे बाह्म विषयों के स्पर्श से विक्षुब्ध नहीं होते। उसका कर्म मात्र शरीरिक कर्म होता है क्योंकि वाकी सब कुछ तो ऊपर से आता है, मानव स्तर पर पैदा नहीं होता, भगवान् पुरुषोत्तम के संकल्प, ज्ञान और आनंद का प्रतिबिंबमात्र होता है ; इसलिये वह कर्म और उसके उद्देश्यों पर जोर देकर अपने मन और हृदयों में वे प्रतिक्रियाएं नहीं होने देता जिन्हें हम षड़रिपु और पाप कहते हैं।
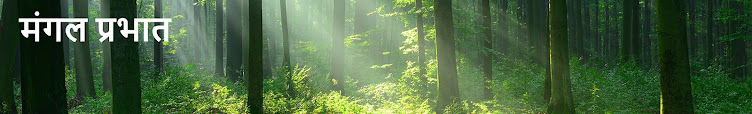
.jpeg)







