यदि कोई कर्म बिना प्रयोजन किया जायेगा तो पानी पीटने के[1] समान निष्फल जायेगा, शक्ति का अपव्यय होगा। इसलिए कोई भी कर्म प्रारम्भ करने के पूर्व यह विचार कर लेना चाहिए कि उससे किस प्रयोजन की सिद्धि होगी, उसमें क्या-क्या विघ्न पड़ेंगे और उन विघ्नों को हम कैसे पार करेंगे? वे लोग अधकचरे होते हैं जो निष्काम का नाम सुनकर चौंक जाते हैं।
अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम् ।
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥[2]
प्रत्येक क्रिया का एक परिणाम होता है। दूध का मन्थन करने पर क्रीम निकलती है। दही के मन्थन से नवनीत निकलता है। मन्थन एक कर्म है। यदि आपको यह ज्ञात नहीं कि दूध-दही के मन्थन का परिणाम क्या होगा तो मन्थन-क्रिया निष्फल हो जायेगी। इसलिए कोई कर्म करना हो तो पहले उसका अनुबन्धन समझना चाहिए। अनुबन्ध में चार बातें विचारणीय हैं। पहली बात यह कि हम कर्म के अधिकारी हैं कि नहीं? हमें अमुक कर्म करना चाहिए कि नहीं? अर्थात् उस कर्म में हमारा अधिकार होना चाहिए। दूसरे, कर्म को स्वरूप से जानना चाहिए। कर्म कैसे करना है यह यदि आपको ठीक-ठीक करना नहीं आता, तो उसमें लगकर आप उसको बिगाड़ देंगे। तीसरे, कर्म के प्रयोजन का विचार करना चाहिए। चौथे यह देखना चाहिए कि उस कर्म के साथ हमारा क्या सम्बन्ध है। इस प्रकार अधिकार, विषय, प्रयोजन और सम्बन्ध इन चारों के ज्ञान का नाम अनुबन्ध है।
कोई भी काम प्रारम्भ करने के पूर्व इन चारों बातों पर विचार कर लो। क्षय का अर्थ हानि। अर्थात यह काम करने में हमें अथवा दूसरों को कितनी हानि पहुँचेगी? पौरुषम का अर्थ है पुरुषार्थ। अर्थात इस काम को पूरा करने की शक्ति हममें है कि नहीं। जो लोग इन बातों का विचार किये बिना केवल मोहवश कर्म प्रारम्भ कर देते हैं, उनका कर्म तमोगुणी हो जाता है। तात्पर्य यह कि उनको अन्त में निष्फलता प्राप्त होती है और कर्म करने का आनन्द भी नहीं मिलता। अब आप इन चारों बातों की कसौटी पर विचार कीजिये। आप कोई कर्म कर लेने के बाद थकान का अनुभव करते है या प्रसन्नता का? यदि आपको प्रसन्नता हो तो समझिये आपने अच्छा काम किया। ग्लानि हो तो समझिये आपका वह काम अच्छा नहीं। मनुस्मृति में कर्म के सम्बन्ध में यह कहा गया है- यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्परितोषो चांतरात्मन। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत् ॥[1] कर्म के साथ आत्मतुष्टि आवश्य होनी चाहिए। कर्म करते समय यदि अन्तरात्मा को सन्तुष्टि का अनुभव हो तो उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। जिस कर्म से आत्मग्लानि या पश्चात्ताप होता हो वह नहीं करना चाहिए। काशी में एक महात्मा थे। उनसे किसी ने कर्म के सम्बन्ध में उपदेश करने की प्रार्थना की तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुम अपने कर्म जज स्वयं हो। कोई काम करने के बाद जब तुम्हारी अन्तरात्मा स्वीकार करती है कि तुमने बुरा काम किया तो वह काम संस्कार बनकर तुम्हारे साथ जुड़ जाता है। यदि तुम किसी कृत कर्म को अन्तरात्मा से नहीं बलात् अस्वीकार करोगे तो समष्टि की भावना तुमसे स्वीकृति का हस्ताक्षर ले लेगी। इसलिए यह ध्यान रखो कि कर्म करते समय तुम्हारी अन्तरात्मा सन्तुष्ट हो रही है, प्रसन्न हो रही है, अथवा ग्लानि का अनुभव कर रही है।
मनुस्मृति में यह श्लोक भी आता है-
यमो वौवस्वतो देवो यस्तवैष हृदि स्थित:।
तेन चेद्विवादस्ते मा गगां मा कुरुन् गम:।
आत्मैव देवता: सर्वा सर्वमात्मन्यवस्थितम्।
आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्॥
हमारे हृदय में भगवान आत्मा के रूप में रहते हैं। यदि उनसे तुम्हारा कोई मतभेद नहीं तो न गंगा नहाने की आवश्यकता है और न किसी तीर्थ की यात्रा करने की। अपने आत्मदेव से कोई विवाद नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने ज्ञान और आकांक्षा के अनुसार काम करते हैं तथा हमारे जीवन के साथ जुड़ जाते है तो हमारी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि आप बुद्धि एवं कर्म की तुलना में बुद्धि को ही श्रेष्ठ और कर्म को कनिष्ठ मानते हैं। फिर मुझे ऐसे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं जिनमें हिंसा होती है। आपने मिले-जुले अस्पष्ट वचनों से मेरी बुद्धि मोह-ग्रस्त हो जाती है। कोई निर्णय नहीं कर पाती-
व्यामिश्रेवेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ।
यह प्रसंग पहले भी आ चुका है। आपको बताया जा चुका है कि अर्जुन के इन वचनों से उनका श्रीकृष्ण के प्रति अत्यन्त प्रेम प्रकट होता है। सचमुच एक मित्र जैसे अपने मित्र से बात करता है वैसे ही अर्जुन श्रीकृष्ण से बात कर रहे हैं। बहुत ममता और प्रियता भरी है उनकी बातों में। उत्तर में भगवान ने अर्जुन को दो प्रकार की निष्ठा बतायी। निष्ठा उसे कहते हैं जहाँ हम स्थिर हो जायँ। ‘नि’ का अर्थ है नितरां और ‘ष्ठा’ का अर्थ है डाँवाडोल न होना। स्थान और स्थिति में जो स्थ है वही निष्ठा में भी है। हमारी निष्ठा हो गयी अर्थात हम पक्के हो गये। अब तो यही करेंगे, इसी ढंग से जीवन का निर्वाह करेंगे। इसी कर्म में अपना पौरुष लगायेंगे और इसी से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी। पहले भी कहा जा चुका है कि प्रयोजन पर दृष्टि रखे बिना कोई कर्म नहीं करना चाहिए।
प्रयोजन का अर्थ होता है- अवगतं तद् आत्मनि इष्यते-जिसका अनुभव होने पर हम चाहें कि यह हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहे। प्रयोजन का अर्थ प्रकृष्ट योजना भी है। अतः प्रयोजन को ध्यान में रखकर ही कर्म करना चाहिए, निष्प्रयोजन नहीं।
तो भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दो प्रकार की निष्टा बतायी, वह यह है-
लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ।
यहाँ अर्जुन के लिए अनघ सम्बोधन है। ‘अनघ’ कहने का अभिप्राय यह है कि तुम जो मुझे यह कह रहे हो कि मैं ठीक-ठीक बात न करके तुम्हें भ्रम में डाल रहा हूँ, इसमें तुम्हारा भाव शुद्ध है और जहाँ शुद्ध भाव है वहाँ शब्दावली पर ध्यान नहीं दिया जाता। तुम्हारे शब्द कुछ भी हो, तुम्हारा तात्पर्य यह है कि तुम अपने कर्तवय को तत्त्वतः जानना चाहते हो। इसलिए तुम निष्पाप हो।
इसके बाद श्रीकृष्ण बताते हैं कि निष्ठा के स्वरूप में अन्तर क्यों पड़ता है? एक तो सांख्ययोग की दृष्टि से, दूसरा कर्मयोग की दृष्टि से। सांख्यशास्त्र में जगत् के पदार्थों की गणना की जाती है। पण्डितगण जगत् के पदार्थों की संख्या करते हैं। संख्या का अर्थ है सम्यक्- ख्याति। कोई भी पदार्थ कितने रूपों में ख्यात हो रहा है इसका आकलन। वेदान्ती लोग ख्याति शब्द का अर्थ भ्रम करते हैं। उनके सत्ख्याति, असत्ख्याति, अन्यथाख्याति, आत्मख्याति, अनिर्वचनीयख्याति आदि पारिभाषिक शब्दों का तात्पर्य यह है कि वस्तु वस्तुतः है एक रूप में और प्रकट हो रही है दूसरे रूपों में। सांख्य शब्द का अर्थ संसार के पदार्थों का सम्यक आख्यान है और उसके परिणामस्वरूप विवेक द्वारा अपने आत्मा को अकर्ता एवं असंग जानना सांख्य का सिद्धान्त है। जो लोग बुद्धिमान हैं उनके लिए विवेक द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग सांख्ययोग है और जो लोग प्रयत्न करके, प्रयास करके किसी वस्तु का निर्माण करना चाहते हैं, उनके लिए कर्मयोग का मार्ग है। निर्माण-विभाग है कर्मयोग और प्रमाण-विभाग है सांख्ययोग।
हमारे शास्त्रों में तीन विभाग माने जाते हैं- तत्त्वमीमांसा, प्रमाण-मीमांसा और कर्ममीमांसा। सत्यवस्तु क्या है? यह तत्त्वमीमांसा है, उसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण क्या है? यह प्रमाणमीमांसा है और हमको जिस ढंग में वर्तना चाहिए यह आचार अथवा कर्म-मीमांसा है। कर्म की शैली बताना एक चीज है और उसको समझना दूसरी चीज है। कर्मयोग निर्माण करता है और सांख्ययोग जो वस्तु जैसी है उसको वैसी दिखाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब अन्त में समझना ही है, ज्ञानी की प्राप्त करना है तो कर्म क्यों किया जाये? यह एक शास्त्रीय प्रसंग है कि जब तक हमारे साथ कर्म लगा रहेगा। तब तक वह कुछ बनायेगा कुछ बिगाड़ेगा और हम उसके कर्ता बने रहेंगे, उसके साथ हमारा सम्बन्ध जुड़ा रहेगा और हम उसके कर्ता बने रहेंगे तो उसका फल उत्पन्न होगा और जब फल उत्पन्न होगा तो उसके अनुसार हमें भिन्न-भिन्न योनियों में जाना पड़ेगा, भिन्न-भिन्न रूप ग्रहण करने पड़ेगें, यह काम कैसे होगा, वह काम कैसे होगा और उसका फल कैसे भोगेंगे, यह प्रसंग सामने आता जायेगा। जब कर्म से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा तभी आत्मदेव अपने स्वरूप में स्थित होंगे और ब्रह्म स्वरूप बनेंगे। यदि कर्म से आत्मा का पूर्णरूप से छुटकारा नहीं होगा तो उसकी मुक्ति नहीं होगी और उसको ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नहीं होगी। कर्म होगा तो सुख-दुःख का अनुभव अवश्यम्भावी है। जब कर्म के फल-स्वरूप सुख-दुःख भोगते जायेंगे तो मुक्ति किस बात की हुई? इसलिए जीवन में नैष्कर्ष्य का आना आवश्यक है। अब प्रश्न उठा कि जब नैष्कर्ष्य ही अपेक्षित है तब पहले से ही कर्म क्यों न छोड़ दिया जाये? यह बात ठीक नहीं। यदि तुम्हें नैष्कर्ष्य प्राप्त करना है तो जो आवश्यक कर्म है उन्हें पूरा करना होगा- न कर्मणामनारम्भान्नैष्कमर्यं पुरुषोऽश्नुते । कतिपय मित्र यात्रा करने गये। उनका जो मुखिया था उसने कहा कि भाई जंगल से लकड़ी इकट्ठी करो गाँव से चावल, दाल, हँडिया आदि ले आओ। फिर भोजन पकाकर खायेंगे और खाने के बाद आग बुझा देंगे। इस पर एक ने कहा कि जब अन्त में आग बुझानी ही है तो जलाने की क्या आवश्यकता है? उसकी यह बात ग़लत थी। इसी प्रकार यदि कोई कहे कि जब हमें अन्त में कर्म छोड़ना है तब पहले ही क्यों न छोड़ दें? तो वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता।
क्रम-क्रम से ही सब कुछ करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति यदि कर्म करेगा ही नहीं तो उसके पौरुष का आविर्भाव कैसे होगा? पौरुष का आविर्भाव आवश्यक है। वह सभी मनुष्यों के लिए सम्भव है। क्योंकि सबके हृदयों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का निवास है-
ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
भगवान ने अपने लिए कोई बँगला न बनाकर समस्त प्राणियों के हृदयों को अपना निवास-स्थान बनाया। संसार के सच्चे साधु-सन्त भी ईश्वर की सत्ता और महत्ता के प्रतीक हैं। वे अपने लिए कोई आश्रम न बनाकर समस्त संसार को अपना आवास समझते हैं। कुछ लोग समझते है कि वे मुफ़्त का खाते हैं। परन्तु भिक्षा माँगने में और उसके लिए कहीं-कहीं अपमानित होने में जो श्रम पड़ता है इसे भुक्तभोगी साधु-सन्त ही जानते हैं। यह बात दूसरी है कि उन्हें सुख-दुःख और मानापमान का विशेष विचार नहीं होता। क्योंकि सुख-दुःख तथा मानापमान में जीवन समान रहने से भी जीवन का निर्माण होता है। साधु-सन्तों की सहनशीलता तथा त्याग-वृत्ति एक ओर जहाँ गरीबों को गरीबी में भी जीवन व्यतीत कर सकने का आश्वासन देती है वहाँ श्रीमन्तों को भी विलासिता से बचने तथा संयमित रहने की प्रेरणा प्रदान करती है। इस प्रकार सच्चे साधु-सन्त धनी और निर्धन के मध्य सेतु बनकर उसको समन्वित करने का काम करते रहते हैं।
मनुष्य के भीतर ईश्वर के रूप में एक महान शक्ति विद्यमान है और आपका सम्बन्ध उस महाशक्ति से है जो सारी सृष्टि का संचालन करती है। किन्तु उसका साक्षात्कार तभी होता है जब आप अपने भीतर के पौरुष को जगाते हैं आप जानते हैं पावर-हाउस में बिजली बहुत होती है; परन्तु आपको आपके बल्ब के अनुसार ही प्रकाश मिल पाता है।
आपके जीवन में जितना अधिक पौरुष प्रकट होगा, उतना ही अधिक ईश्वरीय शक्ति का उपयोग आप कर सकेंगे अथवा उन्हें छोड़ भी सकेंगे। बहुत से लोगों में कर्म करने की तो शक्ति होती है पर उसे छोड़ने की शक्ति नहीं होती। ऐसी शक्ति अधूरी है। जो मशीन को बन्द नहीं कर सकते उन्हें चलाने का कोई अधिकार नहीं। हममें भी हर कर्म कर सकने की तरह कर्म छोड़ने की शक्ति का भी जागरण होना चाहिए। कर्म के साथ नैष्कर्ष्य भी होना चाहिए। इसलिए कर्म प्रारम्भ करो और नैष्कर्ष्य की शक्ति का उपार्जन करो- न कर्मणामनारम्भान्नैष्कमर्यं पुरुषोऽश्नुते । न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥[1] यदि कोई कहे कि हम कर्म से संन्यास ले लेंगे तो उससे किसी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। मन में यदि कामना होगी तो वह कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। कामना अपनी दिशा में ले जाती है। वासना तीन प्रकार की होती है। एक होती है आगे की वासना। हम चाहते हैं कि हमको यह फल मिले। दूसरी यह होती है कि हमारा कर्म पूरा हो जाये और तीसरी यह होती है कि हम हमेशा कर्म करते रहें। इनमें अन्तर होता है। एक मनुष्य ऐसा है जिसके भीतर वासना भी है और कर्म भी है; वह साधारण मनुष्य की तरह काम कर रहा है। यदि कोई कहे कि हम कर्म तो नहीं करेंगे; परन्तु वासना को पड़ी रहने देंगे तो वह भ्रष्ट और मिथ्याचारी हो जायेगा- कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् । इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार: स उच्यते ॥[2] जिसके मन में वासना भरी रहती है और जो बाहर से हाथ-पाँव बाँधकर बैठे रहते हैं और सिद्ध बनने का स्वांग करते हैं वे मिथ्याचारी अथवा ढोंगी कहलाते हैं। यदि कोई ईमानदारी से वासना को मिटाना चाहता है तो वह साधक है। एक मनुष्य कर्म तो करता है, परन्तु उसके भीतर वासना नहीं, वह बहुत श्रेष्ठ है, मुमुक्षु है। सिद्ध पुरुष है जिसमें न कर्म है, न वासना।
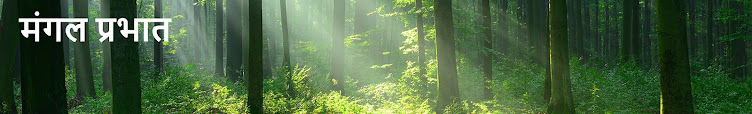
.jpeg)







