गुरु अर्जुन की कठिनाइयों का पहला उत्तर संक्षेप में दे चुके, अब वे दूसरे उत्तर की ओर मुड़ते है और उनके पास से एक आध्यात्मिक समाधान करने वाले जो पहले शब्द निकलते हैं उनमें तुरंत वे यह बताते हैं कि सांख्य और योग में एक भेद है, जिसको जान लेना गीता को समझने के लिये अत्यंत आवश्यक है। भगवान् कहते हैं कि “यह बुद्धि (अर्थात् वस्तुओं और संकल्प का बुद्धिगत ज्ञान) तुझे सांख्य में बता दी, अब इसे योग में सुन, इस बुद्धि से यदि तू योग में स्थित रहे, तो तू कर्म बंधन को छुड़ा सकेगा।“ जिन शब्दों से गीता इस भेद को सूचित करती है उनका यह शब्दश: अनुवाद है। गीता मूलतः वेदांत-ग्रंथ है; और साथ ही साथ उस समय
परिमंडल में व्याप्त अन्य मतों और पंथों का समुचित समाकलन करने का एक सफल और कुशल प्रयास
भी। वेदांत के जो तीन सर्वमान्य प्रमाण ग्रंथ हैं उनमें से गीता है। श्रुति में अवश्य ही इसकी गणना नहीं की जाती, क्योंकि इसकी प्रतिपादन शैली बहुत कुछ बौद्धिक,तार्किक और दार्शनिक है, फिर भी इसका आधार परम सत्य [1] ही है, लेकिन यह वह श्रुति, वह मंत्रदर्शन नहीं है जो ज्ञान की उच्च भूमिका में द्रष्टा को स्वतः प्राप्त होता है [2]तथापि इसका इतना अधिक आदर है कि यह ग्रंथ लगभग तेरहवीं उपनिष्द के रूप में ही स्वीकार्य
एक पवित्र ग्रंथ के रूप में मान्य है |
परंतु इसके वैदांतिक विचार आरंभ से अंत तक सांख्य और योग के विचार से अच्छी तरह समपृक्त हुए हैं और इस संपन्नता के कारण इसके दर्शन पर एक विलक्षण समन्वय की छाप स्वतः सिद्ध रूप से आ गयी है। वास्तविकता यह भी है कि यह मूलतः योग (याग के साथ होने वाले अन्य सभी मतों पंथों और विचार समाकलनों के साथ) की क्रियात्मक पद्धति का उपदेश है, और जो तात्विक विचार (सांख्य, योग, वेदांत और उपनिषद् के विविध अंश आदि ; कहीं कहीं पर स्वतंत्र रूप से और कहीं कहीं पर सम्मिलित रूप से) इसमें आये हैं; विवेचित हुए हैं और हर प्रकार से वेदांत के आधार पर एकरूपता के सिद्धांत से परिपूर्ण रूप से समपृक्त हुए हैं; वे इसके योग की व्यावहारिक व्याख्या [3]करने के लिये किए गये होंगे ऐसा मानना चाहिए | यह केवल वेदांत-ज्ञान का ही निरूपण नहीं, बल्कि कर्म को ज्ञान और भक्ति की नींव पर खड़ा करती और फिर कर्म को उसकी परिणति ज्ञान तक उठाकर उसे भक्ति से अनुप्राणित करती है जो कर्म का हृदय और उसके भाव का भी सारतत्व है; अपितु कर्म को भक्ति और ज्ञान का आधार[4] मिलने से उसमें आनेवाली पवित्रता, निष्ठा और कर्तव्यपरायणता का भी बखान करती है | फिर गीता का योग विश्लेषणात्मक सांख्यदर्शन पर स्थापित है, सांख्य को वह अपना आरंभस्थल बनाता है और उसकी पद्धति और उसके मत में सांख्य को बराबर ही एक बड़ा स्थान प्राप्त है, तथापि गीता का यह योग सांख्य के बहुत आगे जाता है, यहाँ तक कि सांख्य की कुछ विशिष्ट बातों को अस्वीकार करके यह एक ऐसा उपाय बताता है जिससे सांख्य विश्लेषणात्मक कनिष्ठ ज्ञान के साथ उच्चतर समन्वयात्मक और वैदांतिक सत्य का सम्मिलन साधित होता है।
यहाँ इतना कह देना इसलिये आवश्यक है कि उन परिचित शब्दों के प्रयोग से कोई भ्रम उत्पन्न न हो जो यहाँ अपने परिचित और रूढ़ अर्थ की अपेक्षा अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। फिर भी सांख्य और योग दर्शनों में जो कुछ सारत्व है अर्थात् जो कुछ व्यापक, उदार और सर्वमान्य सत्य है वह गीता मे स्वीकृत है, लेकिन गीता इन परस्पर-विरोधी दर्शनों के समान केवल उन्हीं सत्यों से आबद्ध और सन्निविष्ट न रहते
हुए एक सर्वमान्य परिधि में व्याप्त शाश्वत सत्य की प्रतिष्ठा हेतु कटिबद्ध रहने का
प्रयत्न स्वरूप है; इसका सन्नकय भी उदार और वेदांत मान्य सांख्य है | यह वह सांख्य है जिसके प्रथम सिद्धांत और तत्त्व उपनिषदों के वैदांतिक समन्वय में पाये जाते हैं और जिसका वर्णन बाद के विकास में अर्थात् पुराणों में भी आया है। [5]गीता का योग वह आत्मनिष्ठ साधना और आतंरिक परिवर्तन है जो आत्मा को ढूढ़ निकालने या भगवान् से एकता लाभ करने के लिये आवश्यक है और राजयोग इसका एक विशिष्ठ प्रयोग मात्र है। गीता का आग्रह है कि सांख्य और योग परस्पर भिन्न, विसंगत और विरोधी शास्त्र नहीं है, बल्कि दोनों का सिद्धांत और उद्देश्य एक है, भेद केवल उनकी प्रक्रिया और मार्गारंभ में है। सांख्य भी योग है पर यह केवल ज्ञानमार्ग से आगे बढ़ता है, अर्थात् इसका आरंभ हमारी सत्ता के तत्त्वों के बौद्धिक विवेक और विश्लेषण द्वारा होता है और अंत में यह सत्य का दर्शन कर उस पर अधिकार प्राप्त करके अपने लक्ष्य तक पहुँचता है।
दूसरे ओर, योग कर्ममार्ग से अग्रसर होता है ; इसका प्रथम सिद्धांत है कर्मयोग; परंतु गीता की संपूर्ण शिक्षा से तथा कर्म शब्द की जो परिभाषा पीछे की गयी है उसे स्पष्ट है कि कर्म शब्द का प्रयोग गीता में बहुत व्यापक आदि में लिखा गया है और योग शब्द से गीता का अभिप्राय है एक ऐसा निस्वार्थ समर्पण जिसमें हमारी समस्त आंतरिक और बाह्म कर्मण्यताओं को यज्ञ-रूप से कर्म के ईश्वर को,उस सनातन परब्रह्म को भेंट कर देना होता है जो जीव को समस्त ऊर्जा और तपस्या के स्वामी है। यह योग उस सत्य की साधना है जिसका दर्शन ज्ञान से होता है, इस साधाना की प्रेरक-शक्ति है एक प्रकाशमान भक्ति का भाव, एक शांत या उग्र आत्मसमर्पण का भाव उस परमात्मा के प्रति जिन्हें ज्ञान पुरुषोत्तम के रूप में देखता है। पर सांख्य के सत्य क्या हैं ? सांख्य-दर्शन का यह नाम उसकी विश्लेषण-पद्धति के कारण पड़ा है; सांख्या में हमारी सत्ता के तत्त्वों का विश्लेषण, संख्याकरण, विभाजन और विवेचन है, जिनके संघात या संघात के फल को ही मनुष्य की साधारण बुद्धि देख पाती है। सांख्य-दर्शन ने समन्वय-साधना की कोई चेष्टा नहीं की। इस दर्शन का मूलभूत सिद्धांत यथार्थ में द्वैत है, वह आपेक्षिक द्वैत नहीं जो वेदांत का महत्त्व, बल्कि यह वह द्वैत है जो सर्वथा निरपेक्ष और निराला है।
इस सिद्धांत के अनुसार जगत् कारणस्वरूप कोई एक ही सत्ता नहीं है, बल्कि दो मूलतत्त्व हैं जिनका संयोग ही इस जगत् का कारण है-एक है पुरुष जो अकर्ता है और दूसरी है प्रकृति जो कत्री है। पुरुष आत्मा है, साधारण और प्रचलित अर्थ में नहीं, बल्कि उस सचेतन सत्ता के अर्थ में जो अचल, अक्षर और स्वयं-प्रकाश है। प्रकृति है ऊर्जा और उसकी प्रक्रिया। पुरुष स्वयं कुछ नहीं करता, पर वह ऊर्जा और उसकी प्रक्रिया को आभासित करता है; प्रकृति जड़ है पर पुरुष में आभसित होकर वह अपने कम में चैतन्य का रूप धारण कर लेती है और इस प्रकार सृष्टि, स्थिति और संहार अर्थात् जन्म, जीवन और मरण, चेतना और अवचेतना, इंद्रियगम्य और बुद्धिगम्य ध्यान तथा अज्ञान, कर्म और अकर्म, सुख और दु:ख, ये सब घटनाएं उत्पन्न होती है और पुरुष प्रकृति के प्रभाव में आकर इन सबको अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। वास्तव में ये उसके अंग नहीं है बल्कि प्रकृति की क्रिया और गति के अंग हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है; सत्त्व ज्ञान का बीज है, यह ऊर्जा के कर्मो की स्थिति रखता है; रज शक्ति और कर्म का बीज है, यह शक्ति की क्रियाओं की सृष्टि करता है तमस जड़त्व और अज्ञान का बीज है, यह सत्त्व और रज का अपलाप है; जो कुछ वे सृष्टि करते तथा जिसकी वे स्थिति रखते हैं उसका यह संहार करता है।
प्रकृति के ये तीन गुण जब साम्यवस्था में रहते हैं तब सब कुछ जहां-का-तहां पड़ा रहता है, कोई गति, कर्म या सृष्टि नहीं होती। इसलिये चिन्मय आत्म की अचर ज्योतिर्मय सत्ता में आभासित या प्रतिबिंबित होने वाली भी कोई वस्तु नहीं होती। पर जब यह साम्यावस्था विक्षुब्ध हो जाती है तब तीनों गुण परस्पर विषम हो उठते हैं और वे एक दूसरे से संघर्ष करते और एक-दूसरे पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न करते हैं, और उसी से विश्व को प्रकटाने वाला यह सृष्टि, स्थिति और संहार का विरामरहित व्यापार आरंभ होता है। यह कर्म तब तक होता रहता है जब तक पुरुष अपने अंदर इस वैषम्य को, जो उसके सनातन स्वभाव को ढक देता और उस पर प्रकृति के स्वभाव को आरोपित करता है, प्रतिभासित होने देता है। पर जब पुरुष अपनी इस अनुमति को हटा लेता है तब तीनों गुण फिर साम्यावस्था को प्राप्त हो जाते हैं और पुरुष अपने सनातन अविकार्य अचल स्वरूप में लौट आता है, वह विश्व–प्रपंच से मुक्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि अपने अंदर प्रकृति को आभासित होने देना और यह अनुमति देना या लौटा लेना ही पुरुष की एकमात्र शक्ति, है। प्रकृति को अपने अंदर आभासित देखने के नाते पुरुष गीता की भाषा में साक्षी और अनुमति देने के नाते अनुमंता है, पर सांख्य के अनुसार वह कर्ता रूप से ईश्वर नहीं है। उसका अनुमति देना भी निष्क्रीय है और उस अनुमति को लौटा लेना एक दूसरे प्रकार की निष्क्रियता है।
कर्ममात्र ही, चाहे वह आत्मनिष्ठ हो या वस्तुनिष्ठ, आत्मा का स्वधर्म नहीं, उसमें न कोई सकर्मक संकल्प है न कोई सकर्मक बुद्धि। इसलिये पुरुष अकेला ही इस जगत् का कारण नहीं हो सकता, और काई दूसरा कारण भी है यह स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। केवल पुरुष ही अपने चिन्मय ज्ञान, संकल्प और आनंद के स्वभाव से जगत् का कारण नहीं है, बल्कि पुरुष और प्रकृति दोनों की द्विविध सत्ता ही जगत्त का कारण है, एक है निष्क्रिय चैतन्य और दूसरी है गतिशील ऊर्जां। जगत् के अस्तित्व के विषय में सांख्य की व्याख्या उक्त प्रकार की है। परंतु तब ये सचेतन बुद्धि और सचेतन संकल्प कहाँ से आते हैं जिन्हें हम अपनी सत्ता का इतना बड़ा अंग अनुभव करते हैं और जिन्हें हम सामान्यतः और सहज ज्ञान से ही प्रकृति की कोई चीज न मानकर पुरुष की ही मानते है? सांख्य के अनुसार बुद्धि और संकल्प सर्वथा प्रकृति की यांत्रिक ऊर्जा के अंग हैं, पुरुष के गुणधर्म नहीं; ये दोनों ही बुद्धि-तत्त्व है जो जगत् के चौबीस तत्त्वों में से एक तत्त्व है।
इस सृष्टि के विकास के मूल में प्रकृति अपने तीनों गुणों सहित सब पदार्थों की मूल वस्तु के रूप में अव्यक्त अचेतन अवस्था में रहती है फिर उसमें से क्रमशः ऊर्जा या जड़त्व, क्योंकि सांख्य-दर्शन में ऊर्जा और महाभूत एक ही चीज हैं-के पांच मूल तत्त्व प्रकट होते हैं। इनको प्राचीन शास्त्रों में पंचमहाभूत कहा है, ये है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पर यह याद रहे कि आधुनिक सायंस की दृष्टि में ये मूलतत्त्व नहीं है, बल्कि ये जड-प्राकृतिक शक्ति की ऐसी अति सूच्क्ष्म अवस्थाएं हैं जिसका विशुद्ध स्वरूप इस स्थूल जगत् में कहीं भी प्राप्त नहीं। सब पदार्थ इन्हीं पांच सूच्म तत्त्वों के संघात से उत्पन्न होते हैं। फिर इन पंचमहाभूतों में से, प्रत्येक से एक-एक तन्मात्रा उत्पन्न होती है। ये पंचतन्मात्राएं है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन्हीं के द्वारा ज्ञानेन्द्रियों को विषयों का ज्ञान होता है। इस प्रकार मूल प्रकृति से उत्पन्न इन पंचमहाभूतों और उनकी इन पंचतन्मात्राओं से, जिनके द्वारा स्थूल का बोध होता है, उसका विकास होता है जिसे आधुनिक भाषा में विश्व-सत्ता का वस्तुनिष्ठ पक्ष कहते हैं। तेरह तत्त्व और हैं जिनसे विश्व-ऊर्जा का आत्मनिष्ठ पक्ष निर्मित होता है- बुद्धि या महत्, अहंकार, मन और उसकी दस इन्द्रियां(पांच ज्ञानेन्द्रियां और पांच कमेन्द्रियां)।
मन मूल रूप से सभी इंद्रियों और इंद्रिय जन्य क्रियाओं का नियंता है, यह बाह्म पदार्थों का अनुभव करता और उन पर प्रतिक्रिया करता है; क्योंकि इसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों क्रियाएं साथ-साथ होती रहती हैं; इन्द्रियानुभव के द्वारा यह उन अर्थों को ग्रहण करता है जिन्हें गीता में “बाह्म स्पर्श” कहा गया है और उनके द्वारा जगत् को जनता और सक्रिय प्राणशक्ति द्वारा उस पर प्रतिक्रिया करता; प्रतिसाद देता और अन्य सभी संवेदनाओं को आत्मसात करता है। परंतु पांच ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जिनके विषय हैं, यह अपनी ग्रहण करने की अति सामान्य क्रियाओं को विशेष रूप से चलाता है; इसी प्रकार पांच कर्मेन्द्रियों की सहायता से वाणी, गति, वस्तुओं के ग्रहण, विसर्जन और प्रजनन के द्वारा यह प्रतिक्रिया करने वाली कतिपय प्राणी की आवश्यक क्रियाओं को विशेष रूप से चलाता है। बुद्धि जो विवेक-तत्त्व है, वह एक ही साथ बोध और संकल्प दोनों है, यह प्रकृति की वह शक्ति है जो विवेक के द्वारा पदार्थों को उनके गुण-धर्मानुसार पृथक करती और उनमें संगति बैठाती है। अहंकार बुद्धि का अहं‘-पद-वाच्य वह तत्त्व है जिससे पुरुष प्रकृति और उसी क्रियाओं के साथ तादात्म्य पाने की ओर विकसित होता और क्रमिक पप्रोन्नति की ओर बढ़ते रहता है | परंतु ये आत्मनिष्ठ करण उतने ही यांत्रिक हैं, भौतिक संवेदनाओं से ग्रसित हैं[6]; सर्वव्यापक परम पुरुष की सत्ता से बेख़बर हैं और अपने संकीर्ण मानसिकता और भोगवाद के आधार पर क्रियाशील रहते हैं | अचेतन प्रकृति उतने ही अंश हैं जितने कि उसके वस्तुनिष्ठ करण।
यदि हमारी समझ में यह बात न आती हो कि केसे बुद्धि और मन जड़ प्रकृति के अंश हैं या स्वयं जड़ हैं तो हमें इतना ही याद रखना चाहिये कि आधुनिक सायंस को भी यही सिद्धांत ग्रहण करना पड़ा है। परमाणु की अचेतन क्रिया में भी एक शक्ति होती है जिसे अचेतन संकल्प ही कह सकते हैं, प्रकृति के सब कर्मों में यही व्यापक संकल्प अचेतन रूप से बुद्धि का काम करता है। हम लोग जिसे मानसिक बुद्धि कहते हैं वह तत्त्वत: ठीक वही चीज है, जो इस जड़-प्राकृतिक विश्व के सब कार्यों मे अवचेतन रूप से विवेक करने और संगति मिलाने का काम किया करती है। और आधुनिक सायंस यह दिखलाने का यत्न करती है कि मनुष्य के अंदर जो सचेतन मन है वह भी अचेतन प्रकृति के जड़ कर्म का ही परिणाम और प्रतिलिपि है। परंतु आधुनिक विज्ञान जिस विषय को अंधेरे में छोड देता है अर्थात् किस प्रकार जड़ और अचेतन सचेतन का रूप धारण करता है, उसे सांख्यशास्त्र समझा देता है। सांख्य के अनुसार इसका कारण है प्रकृति का पुरुष में प्रतिभासित होना; पुरुष के चैतन्य का प्रकाश जड़ प्रकति के कर्मों पर आरोपित होता है और पुरुष साक्षी-रूप से प्रकृति को देखता और अपने-आपको भूलता हुआ प्रकृति द्वारा प्रेरित भाव से विमोहित होकर यह समझता है कि मैं ही सोचता, अनुभव करता और संकल्प करता हूं, मैं ही सब कार्मों का कर्ता हूं, जबकि यथार्थ में ये सब कर्म प्रकृति और उसके तीन गुणों द्वारा जरा भी नहीं। इस मोह को दूर करना प्रकृति और उसके कर्मों से आत्मा के मुक्त होने का प्रथम सोपान है।
अवश्य ही हमारे इस जगत् में बहुत-सी चीजें हैं जिन्हें सांख्य शास्त्र निरूपित नहीं करता है और कराता भी है तो पूर्ण समाधान कारक रीति से नहीं, परंतु यदि हम जो कुछ चाहते है वह इतना ही है कि हम केवल यौक्तिक व्याख्या द्वारा यह समझ लें कि इस विश्व की प्रक्रियाएं तत्त्वतः क्या है जिसमें हम उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें जो सभी प्राचीन दर्शनों का लक्ष है, अर्थात विश्व-प्रकृति के जंजाल से आत्मा की मुक्ति, तब तो सांख्य का जगत्-निरूपण और मुक्ति का मार्ग उतना ही उत्तम और प्रभावकारी है जितना कि कोई अन्य मार्ग। यहाँ जो बात पहले समझ में नहीं आती वह यह है कि सांख्य प्रकृति को एक, और पुरुष को अनेक मानकर अपने द्वैत सिद्धांत में बहुत्व की स्थापना किसलिये करता है। ऐसा मालूम होता है कि एक ही प्रकृति और एक ही पुरुष को मानने से भी विश्व की सृष्टि और उसके प्रसारण की व्याख्या की जा सकती थी। परंतु पदार्थों के मूल तत्त्वों के निरीक्षण की कठोर विश्लेषण-पद्धति के फलस्वरूप पुरुष-बहुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करना सांख्य के लिये अनिवार्य था। पहली बात यह है कि हम इस संसार में अनेक सचेतन प्राणियों को देखते हैं और इनमें से प्रत्येक इस जगत् को अपने ही ढंग से देखता है और इसकी आंतरिक और बाह्म वस्तुओं को अपने ही ढंग से देख अनुभव करता है।
यद्धपि अनुभव करने वाली तथा प्रतिक्रिया करने वाली क्रियाएं एक ही हैं फिर भी प्रत्येक प्राणी इसके साथ पृथक-पृथक रूप से व्यवहार करता है। पुरुष यदि एक ही होता तो यह केन्द्रीय स्वातंत्रय और पार्थक्य न होता, सभी प्राणी जगत् को एक-सा अनुभव करते और देखते, एक ही रूप में पदार्थ को ग्रहण करते और सबका व्यवहार उनके साथ एक-सा ही होता। चूंक प्रकृति एक है, इसलिये सब प्राणी उसी एक जगत् को देखते हैं; और चूंकि उसके तत्त्व हर जगह एक ही है इसलिये जिन सर्वसाधारण तत्त्वों के कारण आंतरिक और बाह्म अनुभूतियां होती हैं वे भी सबके लिये एक-सी हैं; परतु इन प्राणियों की दृष्टि, विचार और रुख में तथा इनके कर्म, अनुभव और अनुभव से भागने की वृत्ति में जो असंख्य भेद हैं-अवश्य ही ये भेद प्रकृति की स्वाभाविक क्रिया के नहीं, बल्कि साक्षी चेतना के हैं-इस विषय की इसके सिवाय और कोई व्याख्या नहीं हो सकती कि बहुत-से साक्षी हैं, अनेक पुरुष हैं। हम कह सकतें हैं कि पृथक्त्व धर्मवाला अहंकार ही कारण है, यही इस विषय का पर्याप्त उत्तर है। पर अहंकार तो प्रकृति का एक तत्त्व है जो सबके लिये समान है, उसमें भेद होना जरूरी नहीं हैं। वह स्वयं तो केवल इतना ही करता है कि पुरुष को प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेने में प्रवृत्ति करे, और यदि एक ही पुरुष होता तो सब जीव एक होते, अपनी अहंभावमयी चेतना में जुटे हुए और एक-से होते।
उनके रूपो में और उनके प्राकृतिक अंगों के संघातों के व्योरे में चाहे कितना भी भेद होता तो भी जीव पर पड़ने वाले जगत्-दृश्य का असर भिन्न-भिन्न प्रकार का न होता और सबकी अनुभूति भिन्न-भिन्न प्रकार की न होती। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन से एक साक्षी या ऐसे पुरुष में यह केन्द्रित भेद, यह दृष्टयंतर और अथ से इति पर्यन्त अनुभूति का यह पार्थक्य न होना चाहिये था। इसलिये वेदांत के पुरातन ज्ञान से निकली हुई,पर पीछे उससे विच्छित्र, सांख्य की पद्धति में बहु पुरुष का सिद्धांत एक न्याय-संगत आवश्यकता थी। विश्व और उसकी प्रकिृया का एक पुरुष और एक प्रकृति का व्यापार कहकर समझाया जा सकता है, किंतु इससे विश्व में सचेतन जीवों की बहुलता का समाधान नहीं होता। फिर इतनी ही बड़ी एक और कठिनाई है। अन्य दर्शनों की तरह सांख्य ने भी अपना लक्ष “मोक्ष” ही रखा है। हम कह आये हैं कि यह मोक्ष, पुरुष द्वारा प्रकृति के कर्मों से अपनी अनुमति हटा लेने से प्राप्त होता है, क्योंकि प्रकृति के ये कर्म उसी को आनंद देने के लिये है। परंतु, वास्तव में, यह कहने का एक ढंग है। पुरुष अकर्ता है और अनुमति देने या हटा लेने की जो क्रिया है वह यथार्थ में पुरुष की नहीं हो सकती, बल्कि यह अवश्य ही, स्वयं प्रकृति में होने वाली ऐसी गति है। विचार करने से मालूम होगा है कि यह भी बुद्धितत्त्व में-विवेकशील संकल्प में-होने वाली एक क्रिया है, उसकी एक प्रतिक्षेपक या प्रत्यावर्तनकारी गति मात्र है।
बुद्धि ही मन के द्वारा होने वाली विषय-प्रतीत से अपना संबंध जोड़ती रही है; बुद्धि ही विश्व-प्रकृति के द्वारा होने वाले कर्मों का व्यतिरेक और अन्वय करती और अहंकार की सहायता से प्रकृति के विचार, अनुभव और कर्म के साथ द्रष्टा पुरुष का तादात्म्य- साधन करती रही है। यही बुद्धि फिर विवेक द्वारा इस कटु और विघटनात्मक अनुभूति को प्राप्त होती है। कि प्रकृति के साथ पुरुष का तादात्म्य केवल भ्रम है; अंत में इसको यह विवेक होता है कि पुरुष प्रकृति से अलग है और यह सारा विश्वप्रपंच प्रकृति के गुणों की साम्यावस्था का विक्षोभमात्र है। तब बुद्धि, जो एक ही साथ बुद्धि और संकल्प-शक्ति भी है, इस मिथ्यात्व से तुरंत हट जाती है जिसका वह अब तक पोषण करती रही है, और पुरुष बंधन-मुक्त हो जाता है और विश्वप्रपंच में रमने वाले मन का संग नहीं करता। इसका अन्तिम फल यह होता है कि प्रकृति की पुरुष में प्रतिभासित होने की शक्ति नष्ट हो जाती है। क्योंकि अहंकार का प्रभाव अब नष्ट हो गया है और बुद्धि-संकल्प के उदासीन हो जाने के कारण प्रकृति की अनुमति का साधन नहीं रहता: तब अवश्य ही उसके गुण आप ही साम्यावस्था को प्राप्त होगें, विश्व-प्रपंच बंद हो जायेगा और पुरुष को अपनी अचल शांति में लौट जाना होगा। परंतु यदि पुरुष एक ही होता तो बुद्धि-संकल्प के भ्रम से निवृत्त होते ही सारा विश्व-प्रपंच बंद हो जाता। पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता।
असंख्य प्राणियों मे से कुछ ही मोक्ष को प्राप्त होते या मोक्ष-मार्ग के अनुगामी होते हैं; शेष सब प्राणी जहां-के-तहां रहते हैं और विश्व- प्रकृति की जो क्रीड़ा उनके साथ हो रही है उसमें इस क्षिप्र त्याग से उस प्रकृति को रंचमात्र भी असुविधा नहीं होती जबकि उसका सारा कारबार ही इस कार्य से बंद हो जाना चाहिये था। इसकी व्याख्या के लिये यही कहा जा सकता है कि पुरुष अनेक हैं और वे सब-के-सब स्वतत्र हैं। वैदातिक अद्वैतवाद की दृष्टि के अनुसार यदि इसकी कोई न्याय-संगत व्याख्या हो सकती है तो वह मायावाद है। पर मायावाद को मान लेने पर यह सारा प्रपंच एक स्वप्नमात्र हो जाता है, तब बंधन और मुक्ति दोनों ही अविद्या की अवस्थएं, माया की व्यावहारिक भ्रांतिमात्र हो जाती है; वास्तव में न कोई बद्ध है, न कोई मुक्त। सांख्य जो अधिक थार्थवादी है, सृष्टि-विषयक इस मायिक भावना को स्वीकार नहीं करता कि यह सब दृष्टि भ्रम है। इसलिये यह वेदांत के इस समाधान को स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार भी सांख्यों की जगत्-विशलेषण-पद्धति से प्राप्त निष्कर्षों को ग्रहण करते हुए बहु पुरुष का सिद्धांत अपरिहार्य रूप से मानना पड़ता है। गीता सांख्य के इस विश्लेषण की ग्रहण करके अपना उपदेश आरम्भ करती है और जहाँ वह योग का निरूपण करती है वहाँ भी पहले तो ऐसा दिखायी देता है मानो वह सांख्य के इस विचार को प्रायः पूर्णतया स्वीकार करती है।
वह प्रकृति, उसके चौबीस तीन गुणों और चौबीस तत्त्वों को स्वीकार करती है; प्रकृति द्वारा समस्त कर्मों का होना और पुरुष का अकर्ता होना भी गीता को स्वीकार है; विश्व में अनेक सचेतन प्राणियों का होना भी उसे स्वीकार है अहंकार; का तथा बुद्धि की भेदभाव करने वाली क्रिया का लय और प्रकृति के गुण-कर्म का अतिक्रमण ही मोक्ष का साधन है, इसको भी गीता स्वीकार करती है। आरंभ से ही अर्जुन से जिस योग की साधना करने को कहा जा रहा है, वह है बुद्धियोग। परंतु एक महत्त्वपूर्ण व्यत्यय या भेद है। यहाँ पुरुष एक है, अनेक नहीं। गीता का मुक्त, शरीर, अचल, सनातन, अक्षर पुरुष केवल एक बात को छोड़कर और सब बातों मे वेदांत की भाषा मे सांख्यों का ही सनातन, अकर्ता, अचल, अक्षर पुरुष है। पर बहुत बड़ा भेद यही है कि यह पुरुष एक है, बहु नहीं। इससे वह बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है जिसको सांख्य का बहुपुरुषवाद टाल जाता है, और फिर किसी सर्वथा नये समाधान की आवश्यकता खड़ी हो जाती है। गीता यह समाधान, अपने वैदांतिक सांख्य में वैदांतिक योग के सिद्धांतों और तत्त्वों को लाकर करती है। जो पहला नया महत्त्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ प्राप्त होता है वह स्वयं पुरुष के संबंध में है। प्रकृति कर्म का संचालन करती है पुरुष के आनंद के लिये। पर यह आनंद केसे साधित होता है?
सांख्यों के विश्लेषण में इस आनंद के साधन में शांत साक्षी की निष्क्रिय अनुमति मात्र ही कारण है; निष्क्रिय रहकर साक्षी पुरुष बुद्धि और अहंकार के कार्य में अनुमंता होता है और निष्क्रिय रहकर ही वह उस बुद्धि के अहंकार से अलग हट जाने में अनुमति देता है। पुरुष द्रष्टा है, अनुमति का मूल कारण है, अभ्यास के द्वारा प्रकृति के कर्म को धारण करने वाला है,-इस प्रकार साक्षी, अनुमंता और भर्ता है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। परंतु गीतोकक्त पुरुष प्रकृति का प्रभु भी है, वह ईश्वर है। जहाँ संकल्पात्मक बुद्धि का संचालन प्रकृति के हाथ में है, वहाँ सचेतन पुरुष ही सक्रिय रूप से इसका प्रवर्तन करता और इसे शक्ति देता है; वहीं प्रकृति का प्रभु है। जहाँ संकल्पात्मक बुद्धि के कार्य प्रकृति के हैं, वहाँ पुरुष ही सक्रिय रूप से इस बुद्धि को आधार और प्रकाश प्रदान करता है। वह केवल साक्षी ही नहीं, बल्कि ज्ञाता और ईश्वर भी है, ज्ञान और संकल्प का स्वामी भी है। प्रकृति की कर्म में प्रवृत्ति का वही परम कारण है। सांख्यों की विश्लेषणात्मक विवेचन-पद्धति में पुरुष और प्रकृति विश्व के दो कारण हैं; और इस समन्वयात्मक सांख्य में पुरुष, अपनी प्रकृति के द्वारा, विश्व का एकाम कारण है। हम तुरंत देख सकते हैं कि सांख्या-परंपरा की जकड़ी हुई कट्टर पंथी-विश्लेषण-प्रणाली से हम कितनी दूर निकल आये हैं।
परंतु गीता आरंभ से जिस एक, अद्वितीय पुरुष की बात कर रही है जो अक्षर, अचल और नित्य मुक्त है, उसका क्या हुआ? वह अव्यय, अविकार्य, अज, अव्यक्त ब्रह्म है, फिर भी उसी के द्वारा यह सारा विश्व प्रसारित है। इसलिये ऐसा मालूम होगा कि ईश्वर तत्त्व उसकी सत्ता में है; एक और यदि वह अचल है तो दूसरी ओर समस्त कर्मों और गतियों का कारण और प्रभु भी है। पर कैसे? और विश्व में जो अनेक सचेतन प्राणी हैं, कैसे हैं? ये तो ईश नहीं, अनीश ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये त्रिगुण के कर्म और अहंकारजन्य भ्रम के वशीभूत हैं, और यदि ये सब एक ही आत्मा हैं, जैसा कि गीता का आशय मालूम होता है, तो यह प्रकृति में लीनता, वश्यता और भ्रांति कहाँ से उत्पन्न हुई, अथवा इसका सिवाय यह कहने के कि पुरुष सर्वथा निष्क्रिय है, दूसरा क्या समाधान? और, फिर पुरुष का यह बहुत्व कहाँ से आया? अथवा यह क्या बात है कि जहाँ उस एक, अद्वितीय पुरुष की किसी एक शरीर और मन में तो मुक्ति होती है, वहीं अन्य शरीरों और मनों में वह बंधन के भ्रम में बना रहता है? ये शंकाएं हैं जिनका समाधान करना ही होगा, इन्हें यूं ही नहीं टाला जा सकता। गीता के वाद के अध्यायों में इन सब शंकाओं का, प्रकृति और पुरुष के विश्लेषण द्वारा समाधान किया गया है। इस विश्लेषण में कुछ ऐेसे नवीन तत्त्वों का अविष्कार किया गया है जो सांख्य-परंपरा के लिये तो पराये हैं, पर वैदांतिक योग के लिये उपयुक्त हैं।
यहाँ तीन पुरुष या एक पुरुष के तीन पाद कहे गये हैं। उपनिषदो में सांख्य सिद्धांतों का विवेचन करते हुए कभी-कभी दो ही पुरुषों का वर्णन दीख पढ़ता है। एक मंत्र में यह वर्णन है कि एक अजा है जिसके तीन वर्ण हैं, यह प्रकृति के सनातन स्त्री-तत्त्व का वर्णन है जो अपने तीनों गुणों के साथ सतत सृष्टि–कर्म कर रही है; और दो अज हैं, दो पुरुष हैं जिनमें से एक प्रकृति से लिपटा हुआ है और उसे भोगता है, दूसरा उसे त्याग देता है, क्योंकि वह उसके सब भोग भोग चुका है। दूसरे मंत्र में यह वर्णन है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, दोनों एक-दूसरे के सदा से सयूज सखा हैं; एक उस वृक्ष के फल खाता है ( अर्थात् प्रकृतिस्थ पुरुष प्रकृति के विश्व-प्रपंच को भोगता है), दूसरा नहीं खाता, पर अपने सखा को देखता रहता है-यह निश्चल और नीरव साक्षी पुरुष है जो भोग से निवृत्त है; जब पहला दूसरे को देखता और यह जानता है कि सारी महिमा उसी की है तब वह दु:ख से मुक्त हो जाता है। दोनों मंत्रों में विभिन्न दृष्टि से वर्णन किया गया है, पर आशय दोनों का एक है।
उन दो पक्षियों से एक सदा निश्चल-नीरव मुक्त पुरुष है जिसके द्वारा यह विश्व प्रसारित है और जो अपने द्वारा प्रसारति इस विश्व को देाखता है, पर इससे निर्लिप्त रहता है; दूसरा प्रकृतिस्थ पुरुष है। प्रथम मंत्र यह बतलाता है कि दोनों पुरुष एक ही हैं, उसी एक चिदरुप पुरुष की बद्ध और मुक्त इन दो अवस्थाओं को प्रतिभाषित करते हैं; क्योंकि जो दूसरा अज है वह प्रकृति मे उतरकर उसके भोगों को भोगकर उनसे निवृत्त हुआ है। दूसरा मंत्र यह बात बतलाता है जो हमको पहले मंत्र से नहीं मिलती, कि पुरुष अपनी एकत्व की परमाव्स्था में सदा ही मुक्त, अकर्ता और अनासक्त है और केवल अपनी निम्न सत्ता में स्थति होकर प्रकृति द्वारा सृष्ट प्राणियों के बहुत्व में उतर आता है और फिर किसी व्यक्तिभूत प्राणी के द्वारा वापस लौटकर प्रकृति से निवृत्त हो जाता और अपनी उच्चतर अवस्था में आ जाता है। एक ही सचेतन आत्मा की द्विविध अवस्था का यह सिद्धांत एक रास्ता तो खोल देता है, पर एक के अनेक होने की प्रक्रिया अब भी उलझी हुई है। इन दो पुरुषों में, गीता उपनिषदों के अन्य वचनों का आशय विवाद करते हुए एक और पुरुष मिलाती है, जिसकी महिमा यह सारी सृष्टि है। इस प्रकार तीन पुरुष हुए क्षर, अक्षर और उत्तम क्षर क्षरणशील विकार्य प्रकृति है, स्वभाव है; यह जीव की बहुविध संभूति; यहाँ पर जो पुरुष है वह भागवत सत्ता की बहुत्वावस्था है, यही बहुपुरुष है, यह पुरुष प्रकृति से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि यह ‘प्रकृतिस्थ पुरुष’ है।
अक्षर, कूटस्थ अविकाय पुरुष निश्रल-नीरव और निष्ष्क्रिय आत्मा है, यह भागवत सत्ता की एकत्वावस्था [1] है, यहाँ पुरुष प्रकृति का साक्षी है, पर प्रकृति के कार्यों में लीन नहीं, यह प्रकृति और उसके कर्मों से मुक्त, अकर्ता पुरुष है। उत्तम पुरुष परमेश्वर, परब्रह्म, परमात्मा है, जिसमें अक्षर का एकत्व और क्षर का बहुत्व, दोनों ही अवस्थाएं सन्निविष्ट है। वह अपनी प्रकृति की विशाल गतिशीलता और कर्म के द्वारा, अपनी कन्नी शक्ति, अपने संकल्प और सामर्थ्य के द्वारा जगत् में अपने-आपको व्यक्त करता है और अपनी महत्तर निस्तब्धता और अचलता के द्वारा उससे अलग रहता है; फिर भी वह अपने पुरुषोत्तम रूप में, प्रकृति से अलावा और प्रकृति से आसक्ति इन दोनों अवस्थाओं के ही परे है। पुरुषोत्तम की यह भावना यद्यपि उपनिषदों में सवत्र ही अभिप्रेत है, तथापि इसको स्पष्ट और विनिश्रत रूप से गीता ने ही सामने रखा है और भारतीय धार्मिक चेतना के पिछले संस्कारों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। अद्वैतवाद की सूत्रबद्ध परिभाषाओं का अतिक्रम कर जाने का दावा करने वाले उच्चतम भक्तियोग का आधार यही पुरुषोत्तम-भाव है और भक्ति-प्रधान पुराणों के पीछे भी यही भाव है। गीता सांख्यशास्त्र के प्रकृति-विश्लेषण के चौखटे के अंदर भी बंधी नहीं रहती; क्योंकि इस विश्लेषण के अनुसार प्रकृति में केवल अहंकार को स्थान मिलता है, बहुपुरुष को नहीं-वहाँ पुरुष प्रकृति का कोई अशं नहीं, बल्कि प्रकृति से पृथक है इसके विपरीत गीता का सिद्धांत यह है कि परमेश्वर ही अपने स्वभाव से जीव बनता है। यह कैसे संभव है जब विश्व-प्रकृति के चौबीस तत्त्व है, चौबीस छोड़कर कोई पच्चीसवां तत्त्व नहीं? गीता के भगवान् गुरु कहते है कि हां, त्रिगुणात्मिका प्रकृति के बाह्मकर्म का यही सही विवरण है और इस विवरण में पुरुष और प्रकृति का जैसा संबंध बताया गया है, वह भी विल्कुल सही है और प्रवृत्ति या निवृति के साधन में इसका बहुत बड़ा व्यावहारिक उपयोग भी है; परंतु यह त्रिगुणत्मिक अपरा प्रकृति है जो जड़ और बाह्म है, इसके परे एक परा प्रकृति है जो चिस्वरूपा और भागवत-भावरूपा है और यही परा प्रकृति जीव बनी है।
अपना प्रकृति में प्रत्येक जीव अहंकार के रूप में भासित होता है, परा प्रकृति में प्रत्येक जीव व्यष्टिरूप पुरुष है, अर्थात् बहुत्व उस एक का ही आध्यात्मिक स्वभाव है। यह व्यष्टि-पुरुष, भगवान् कहते हैं कि, स्वयं में हूं, इस सृष्टि में मेरा ही आंशिक प्राट्य है, यह मेरा ही अंश है, और इसमें मेरी सब शक्त्यिां मौजूद हैं; यह साक्षी है, अुमंता है, कर्ता है, ज्ञाता है, ईश्वर है। यह अपरा प्रकृति में उतर आता है और यह समझता है कि मैं कर्म से बंधा हूं, इसलिये कि निम्न सत्ता को भोग सके; यह इससे निवृत्त होकर यह जान सकता है कि मैं कर्म के बंधन से सर्वथा विनिर्मुक्त अकर्ता पुरुष हूँ। यह त्रिगुण से ऊपर उठकर और कर्म-बंधन से मुक्त होकर भी कर्म कर सकता है, जैसे भगवान् कहते हैं कि मैं करता हूं, और पुरुषोत्तम की भक्ति पाकर और उनसे मुक्त होकर उनकी दिव्य प्रकृति का पूर्ण आनंद ले सकता है।
गीता का विश्लेषण ऐसा है जो बाह्म सृष्टि-क्रम से ही बद्ध न होकर परा प्रकृति के 'उत्तम रहस्य’ तक में प्रविष्ट हैं उसी उत्तम रहस्य के आधार पर गीता वेदांत, सांख्य और योग का समन्वय, ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय स्थापित करती है। केवल सांख्य-शास्त्र के द्वारा कर्म और भक्ति का समन्वय परस्पर-विरोधी होने से असंभावित है। केवल अद्वैत सिद्धांत के आधार पर योग के अंगरूप से कर्मो का सदा आचरण और पूर्ण ज्ञान, मुक्ति और सायुज्य के बाद भी भक्ति में रमण असंभव है या कम-से-कम युक्ति-विरुद्ध और निष्प्रयोजन है। गीता का सांख्य-ज्ञान इन सब बाधाओं को दूर करता है और गीता का योगशास्त्र इस सब पर विजय लाभ करता है।
[1]
तस्माद् युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदम् जगत् । आत्मनीक्षस्व विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ॥ श्रीमदभागवत ११.
७.९ ॥
शब्दार्थ: तस्मात्—इसलिए; युक्त—वश में लाकर;
इन्द्रिय-ग्राम:—सारी इन्द्रियों को; युक्त—दमन करके; चित्त:—अपना मन; इदम्— यह; जगत्—संसार; आत्मनि—आत्मा के भीतर; ईक्षस्व—देखो; विततम्—विस्तीर्ण (भौतिक भोग की वस्तु के
रूप में); आत्मानम्—तथा उस आत्मा को;
मयि—मुझ; अधीश्वरे—परम नियन्ता में ।
अपनी सारी
इन्द्रियों (कार्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय ) को वश
में करते हुए तथा मन को दमन
करके, तुम सारे विश्व चराचर सृष्टि (जगत ) को आत्मा के
भीतर स्थितहोता हुआ महसूस करो, जो सर्वत्र समान
रूप से प्रसारित भी
है और परिव्याप्त भी| सिर्फ़
इतना ही नहीं, तुम
इस आत्मा को मुझ पूर्ण
पुरुषोत्तम परमेश्वर के
भीतर भी स्थित
होता हुआ महसूस करो |
[2]
आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषत: । यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोऽसावनुविन्दते ॥ श्रीमदभागवत ११.
७.२० ॥
शब्दार्थ : आत्मन:—अपना ही;
गुरु:—उपदेश देने वाला गुरु; आत्मा—स्वयं; एव—निस्सन्देह; पुरुषस्य—मनुष्य का; विशेषत:—विशेष अर्थ में; यत्—क्योंकि; प्रत्यक्ष—प्रत्यक्ष अनुभूति से; अनुमानाभ्याम्—तर्क के प्रयोग से;
श्रेय:—असली लाभ; असौ—वह; अनुविन्दते—प्राप्त कर सकता है
।.
बुद्धिमान व्यक्ति,
जो अपने समझ की सीमा के
अंतर्गत सब ओर परिव्याप्त दृश्य
जगत का अनुभव करने
तथा ठोस तर्क का आधार लेकर
विस्तार और संचरण समझने
में निपुण होता है, अपनी ही बुद्धि के
द्वारा प्रकृत लाभ प्राप्त कर सकता है।
ऐसा करते हुए कभी कभी सम्यक ज्ञान से पुष्ट दिव्य
जीवन का पथिक वैसा मनुष्य
अपना ही उपदेशक गुरु
बन जाता है।
[3]
पुरुषत्वे च मां धीरा:
साङ्ख्ययोगविशारदा: । आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपबृंहितम् ॥ २१ ॥
शब्दार्थ : पुरुषत्वे—मनुष्य-जीवन में; च—तथा; माम्—मुझको; धीरा:—आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से
ईर्ष्या से मुक्त हुए;
साङ्ख्य योग—वैश्लेषिक ज्ञान तथा भगवद्भक्ति से बने आध्यात्मिक
विज्ञान में; विशारदा:—दक्ष; आविस्तराम्—प्रत्यक्षत: प्रकट; प्रपश्यन्ति—वे स्पष्ट देखते
हैं; सर्व—सभी; शक्ति—मेरी शक्ति से; उपबृंहितम्—प्रदत्त, समन्वित ।.
आत्मसंयमी और
सांख्य योग में दक्ष साधक सहज रूप से ईश्वर के
सान्निध्य को उनके सही
स्वरूप के साथ प्रसारित
औट जगत व्यापी हर जीव में
अभिव्यक्त होता हुआ देख सकते हैं और यह भी
अनुभव कर सकता हैं
कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हर एक
अंश सभी जीवों में, सृष्टि के सभी कनों
में अंश रूप में विद्यमान हैं और नियंता ब्रह्म
स्वरूप हैं |
[4]
प्राणवृत्त्यैव सन्तुष्येन्मुनिर्नैवेन्द्रियप्रियै:
। ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत
वाङ्मन: ॥ ३९ ॥
शब्दार्थ: प्राण-वृत्त्या—प्राणों के कार्य करते
रहने से; एव—ही; सन्तुष्येत्—सन्तुष्ट रहना चाहिए; मुनि:—मुनि; न—नहीं; एव—
निस्सन्देह; इन्द्रिय-प्रियै:—इन्द्रियों को तृप्त करने
वाली वस्तुओं से; ज्ञानम्—चेतना; यथा—जिससे कि; न नश्येत—नष्ट
न हो सके; न
अवकीर्येत—क्षुब्ध न हो सके;
वाक्—उसकी वाणी; मन:—तथा मन ।.
मुनि (विद्वान
भक्त, ईश्वर अनुरागी ज्ञानी) भौतिक इंद्रिय द्वारा मिलनेवाले संतुष्टि की खोज में
न रहे; उसे अपपने शरीर का जतन उतना
ही करना चाहिए जेसके करने से उच्चतर ज्ञान
की अनुभूति नष्ट न हो और
वाणी, अनुक्रियाएँ तथा मन कभी भी
आत्म साक्षात्कार के मार्ग से
विचलित न हो पाए
|
[5] विषयेष्वाविशन् योगी नानाधर्मेषु सर्वत: । गुणदोषव्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुवत्
॥ ४० ॥
शब्दार्थ:
विषयेषु—भौतिक वस्तुओं के सम्पर्क में;
आविशन्—प्रवेश करके; योगी—जिसने आत्म-संयम प्राप्त कर लिया है;
नाना धर्मेषु—विभिन्न गुणों वाले; सर्वत:—सर्वत्र; गुण—सद्गुण; दोष—तथा दोष; व्यपेत-आत्मा—वह व्यक्ति जिसने
लाँघ लिया है; न विषज्जेत—नहीं
फँसना चाहिए; वायु-वत्—वायु की तरह ।.
योगी
भी कई भौतिक वस्तुओं
से विविध प्रकार से प्रभावित होते
रहता है ; पर भौतिक अच्छाई
और बुराई लाँघ लेनेवाला साधक उन तमाम भौतिक
वस्तुओं और सुख सिविधाओं
से घिरा रहते हुए भी उनमें लिप्त
नहीं रहकर ठीक वैसा ही कार्य करे
जैसा कि वायु किया
करता है |
[6] विसर्गाद्या: श्मशानान्ता भावा देहस्य नात्मन: ।
कलानामिव
चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवर्त्मना ॥ ४८ ॥
शब्दार्थ
विसर्ग—जन्म; आद्या:—इत्यादि; श्मशान—मृत्यु का समय, जब
शरीर भस्म कर दिया जाता
है; अन्ता:—अन्तिम; भावा:— दशाएँ; देहस्य—शरीर की; न—नहीं; आत्मन:—आत्मा का; कलानाम्—विभिन्न अवस्थाओं का; इव—सदृश; चन्द्रस्य—
चन्द्रमा की; कालेन—समय के साथ; अव्यक्त—न दिखने वाला;
वर्त्मना—गति से ।.
जन्म से लेकर मृत्यु
तक भौतिक जीवन की विभिन्न अवस्थाएँ
उस भौतिक शरीर के ही विविध
गुणधर्म हैं और ये आत्मा
को उसी तरह प्रभावित नहीं करतीं, जिस तरह चन्द्रमा की घटती-बढ़ती
कलाएँ चन्द्रमा को प्रभावित नहीं
करतीं; ऐसे
परिवर्तन सर्वदा ही काल की
गति के द्वारा
अव्यक्त रूप से लागू
किये जाते हैं।
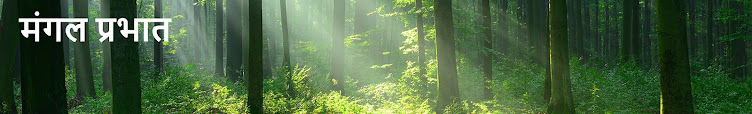








.jpg)