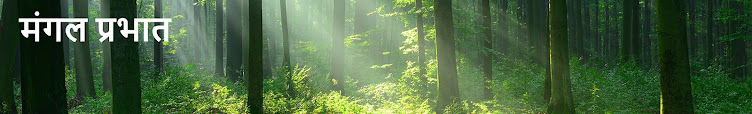यह पहला और सबसे छोटा उपनिषद् शुक्लयजुर्वेद की संहिता का अंतिम अध्याय है। इसे संहितापनिषद् भी कहा जाता रहा। ऐसा इसलिए भी किया गया ताकि इसे अन्य उपनिषदों से अलग किया जा सके, जो ब्राह्मणों में अपना स्थान सुनिश्चित कर लेते है। हिरण्मय पुरुष और विज्ञानमय पुरुष के बीच साम्य, व्यवधान, परस्पर क्रिया और ब्रह्म स्वरुप की अनुभुति का विषय १८ श्लोकों के जरिये बताया गया। सत्य का आश्रय लेनेवालों को मोक्ष पाने का अधिकारी माना गया; व्यक्त के साथ साथ अव्यक्त की उपासना; विद्या के साथ साथ अविद्या की उपासना; स्थूल शरीर के अनित्यता का विषय इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं ।
ईशावास्यमिदं सर्वं
यत्किञ्च जगत्यां जगत् |
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा
मा गृधः कस्य स्विद्धनम् || १ ||
" जगत में जो कुछ
व्याप्त हो रहा है सब उन्हींका (परमेश्वर का) है; अतः त्याग की भावना से इन सबका भोग
करना चाहिए; धन सम्पदा भी उन्हींका और, नहीं तो और किसका है? अतः लालच मत करो; धन किसका
है? अर्थात किसी के पास वैसा धन है ही नहीं जिसको आने के लिए लालच किया जा सके; सबकुछ
ईश्वर के चिंतन करने के लिए त्याग दिया गया हो वह सब आत्मा ही सबकुछ है; अतः यह विचार बनता है कि सब आत्मा
का है और सबकुछ आत्मा का ही है; इसलिए जो असत्य है उसका लालच नहीं करना है। "
कुर्वन्नेवेह कर्माणि
जिजीविषेच्छतं समाः |
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति
न कर्म लिप्यते नरे || २ ||
"यदि कोई इस पृथ्वी
पर सौ वर्ष तक जीवित रहना चाहे तो भी कर्म से छुटकारा पाने का कोई विधान है ही नहीं।
जीते जी कर्म करते ही रहना होगा; कमसे काम विधायक कर्म (यज्ञ , दान और तप) में तो लगे
रहना ही होगा; अन्य कोई उपाय नहीं है। "
असूर्य नाम ते लोका
अन्धेन तमसावृतः |
तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति
ये के चत्महनो जनाः || ३ ||
"असुरों की प्रकृति
वाली योनियाँ अन्धकार से आच्छादित होती हैं;
जो अपनी आत्मा को अधोगति में इ जाते हैं पुनः पुनः शरीर छोड़ने के बाद भी उसी शरीर को
पाते हैं; अतः आध्यात्मिक उन्नति से वंचित रह जाते हैं। "
अनेजादेकं मनसो जावियॉ
नैनाद्देवा आप्नुवनपूर्वमर्षत |
तद्धावतोऽन्यानात्येति
तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्व दधाति || ४ ||
"स्थिर होनेके
साथ साथ यह मन से भी तेज है; इससे भी तेज दौड़नेवाली इन्द्रियाँ इसे पकड़ नहीं पाती;
अपने पीछे दौडनेवालों से भी यह तेज चलता है (स्थिर होनेके साथ साथ। सर्वव्यापी सूत्रात्मा स्वरुप वायु सभी जीवों की
गतिविधियाँ का समर्थक भी है। "
तदेजति तन्नैजति तद्दुरे
तद्वन्तिके |
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु
सर्वस्यस्य बाह्यतः || ५ ||
"वह गतिमान है,
स्थिर भी; दूर है और निकट भी; सबके भीतर है और बाहर भी।"
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति
|
सर्वभूतेषु चैत्मनं
ततो न विजुगुप्सते || ६ ||
" अपनी आत्मा में
सबकुछ देखनेवाले और सबकुछ में अपनी आत्मा को देखनेवाले किसीसे घृणा नहीं करते।
"
यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानातः
|
तत्र को मोहः कः शोक
एकत्वमनुपश्यतः || ७ ||
सा पर्यगाच्छुक्रमकायमवर्णमस्नाविरंशुद्धं
अपापविद्धम् |
कविर्मनीषी परिभूः स्यामभूर्यथाथ्यतोऽर्थान्व्यददच्छश्वतिभ्यः
समाभ्यः || ८ ||
अन्धन्तमः प्रविशन्ति
येऽविद्यामुपासते |
ततो भूय इव ते तमोय
उ विद्यायां रताः || ९ ||
अन्यदेवाहुर्विद्यायान्यादाहुरविद्या
|
इति शुश्रुमा धीराणां
ये नास्तदविकचक्षिरे || १० ||
"ज्ञानी को समस्त
भूत उसकी आत्मा के साथ एकरूप हटा हुआ देख पानेकी स्थिति में फिर कैसा व्याकुलता, कैसा शोक? वह सबमें व्याप्त था,
तेजस्वी, शरीररहित, दोषरहित, स्नायुरहित, शुद्ध, पाप से अछूता; दूरदर्शी, सर्वज्ञ,
दिव्य, स्वयंभू,; न किसी माध्यम से उत्पन्न होनेवाला; विभिन्न सनातन सृष्टिकर्ताओं
को उनके-उनके कार्य को आवंटित करनेवाला । अविद्या की पूजा करनेवाले अंधकार से ग्रसित
होते हैं; केवा विद्या की पूजा करनेवाले और भी घोर अंधकार से ग्रसित हो जाते हैं। एक
परिणाम अविद्या से फलित होता है तो दूसरा विद्या से; ऐसा संत महात्मा सिखाते हैं। "
विद्यां चाविद्यां च
यस्तद्वेदोभ्यं सह |
अविद्याया मृत्युम्
तीर्थ्वा विद्यायामृतमश्नुते || ११ ||
"विद्या और अविद्या
दन्न को जानलेनेवाले विद्या के कारण अमरता पाता है और अविद्या (कर्म स्वरुप प्रवृत्तियां)
से मृत्यु को पर कर लेता है।"
अंधं तमः प्रविशन्ति
येऽसंभूतिमुपासते।
ततो भूय इव ते तमो य
उ संभूत्यं रताः ॥ 12 ॥
“जो अजन्मा प्रकृति की पूजा करते हैं वे अन्धकार
में प्रवेश करते रहते हैं; अज्ञान के घोर अंधकार में; प्रमाद के कराल ग्रास में; दुःख
और दुर्दशा के घोर आवेश में; जो लोग कार्य
ब्रह्म हिरण्यगर्भ पर तुले हुए हैं वे महान् अन्धकार में गिरते हैं । (12)
असंभूतिः वह है जो संभूतिः
(दूसरे से उत्पन्न) न हो; अनिर्मित प्रकृति अर्थात् वह प्रकृति जिसका कोई कारण न हो;
यह अव्यक्त या अव्यक्त प्रकृति है, जिसमें तीनों गुण (सत्व, राजस और तामस के बीच एक
संतुलित स्थिति का होना; एक समन्वय का होना; तीनं गुणों के बीच संतुलन की स्थिति ;
जैसा होने से प्रकृति में उस अवयव क परिव्याप्त होते हुए महसूस नहीं किया जाता होगा
) एक ही अवस्था में रहने का तात्पर्य हुआ गुण साम्यावस्था ; द्रव्य, ऊर्जा तथा नाना प्रकार की ध्वनियाँ अविभेदित
अवस्था में रहती हैं। हिरण्मय पुरुष के प्रभाव से पदार्थ और ऊर्जा के बीच सामंजस्य
विघ्नित होने की स्थिति में सूर्य एक नक्षत्र के रूप में ऊर्जा का विकीरण करते हुए
अन्य सभी कार्यों के कारण स्वरुप बने हुए हैं।
वही हिरण्यगर्भ की भी स्थिति मानी जायेगी; जिसके प्रभाव से अंधकार भी दूर हो
जाता है। यही सबका कारण है। रूप से सृष्टि
के बीजक रूप से रहता है; ठीक जैसे बायवृक्ष की चेतना को बीज में सुप्त अवस्था में पाया
जाता है; सही वातावरण पाते ही प्रस्फुटित होकर चैतन्यमय हो जाता है।
अव्यक्त प्रकृति की उपासना (अव्यक्त-उपासना ) भी
अज्ञान है; इसमें सभी इच्छाओं और कर्मों का बीज निहित है; हिरण्यगर्भ संभूति (कार्य
ब्रह्म) अव्यक्त से उत्पन्न हुआ; अव्यक्त प्रकृति का प्रभाव; एक ऐसी स्थिति जहां तीनों
गुणों के बीच का संतुलन विगणित होजाने की स्थिति में अव्यक्त को जी व्यक्त प्रकृति
के रूप में पाएंगे; हिरण्मय पुरुष और विज्ञानमय पुरुष के बीच में ऊर्जा का संचार शुरू
होगा; चैतन्यमय जीवनचर्या को मूर्त होता हुआ भी पाएंगे।
वह अधिक घने अंधकार
में वह प्रवेश करता है जिसने शून्य होने की कल्पना की है। अस्तित्व में आने से , न
आने से भी भिन्न है; प्राचीन ऋषियों से यह सिद्धांत प्राप्त किया है; जो होने और न
होने दोनों को (अस्तित्वहीन के रूप में) जानता है, वह मृत्यु से परे दोनों से गुजरता
है , और अमरता प्राप्त करता है।
[अव्याकृत (प्रकृति
) और व्यक्त ब्रह्म की उपासना के संयोजन की दृष्टि से , प्रत्येक वैसी क्रिया (व्यक्त
और अव्यक्त के विषय में ध्यान लगाना; उपासना करना; कर्मकांड का अनुष्ठान करना ) अपने
आप में निन्दा योग्य है। " असम्भूतिः " वह है जो दूसरे से उत्पन्न हुआ है;
इसलिए अजन्मा प्रकृति (अज्ञान है, जो सबका कारण है, जिसे अव्याकृत माना गया; जिसकी
उपासना लोग करते हैं; जिसके विविध अवयव और विविध रूप की भी उपासना प्रचलित होती आई
; जो सभी इच्छाओं और कर्मों का बीज है; जो
अपने स्वभाव में केवल अंधा है; वैसी उपासना करनेवाले भी विविध रकार से अंधकार से ग्रसित
होते हैं; उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाति है; उन्हें भी उचित - अनुचित का धयान नहीं
रहता; उन्हें भी अज्ञान रूप प्राद की छाया से ग्रसित रहना पड़ता है; उनके लिए भी सच
और झूठ का सही निर्णय ले पाना कठिन हो जाएगा; कभी कभी दुःसाध्य भी हो जाएगा। हिरण्यगर्भ नामक कार्य-ब्रह्म की उपासना करनेवाले और भी गहन
अंधकार से ग्रसित हो जाते हैं।
अन्यदेवहुः सम्भवादन्यादाहुरसम्भवात्
|
इति शुश्रुमा धीराणां
ये नास्तदविकचक्षिरे || 13 ||
“हिरण्यगर्भ की पूजा
से एक बात फलित होती है और प्रकृति की पूजा से दूसरी बात; बुद्धिमान गुरुओं से ऐसा
कहते सुना ; ऐसी एक अवधारणा भी प्रकृति में व्याप्त हो रही है। हिरण्यगर्भ की उपासना से अणिमा (अणु जैसी स्थिति)
और अव्यक्त राकृति की उपासना से लीनता (प्रकृति में विलीन होना ) साधित हो सकती है।
संभूतिं च विनाशं च
यस्तद्वेदोभयं सह |
विनाशेन मृत्युं तीर्थ्वा
संभूत्यामृतमश्नुते || ईशावास्योपनिषद श्लोक
१४ ||
"एकसाथ उपासना
करनेवाले साधक हिरण्यगर्भ की पूजा से मृत्यु से पार हो जाते हैं और प्रकृति की पूजा
से अमरता भी पाते हैं ; उभय प्रकार से उनकी साधना फलित होगा ।"
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं
मुखम् |
तत्त्वं पुष्पनपावृणु
सत्यधर्माय दृष्टये || ईशावास्योपनिषद श्लोक १५
||।
" सत्य (जिसे परमेश्वर
का स्वरुप भी मानेंगे; जो माया द्वारा रचित संसार से ही परे है; जिसे अव्यक्त प्रकृति
में लीं अवस्था में भी पाते होंगे; जिसका रहस्य उदघाटन करते समय बड़े बड़ी महात्मा भी
भ्रमित हो जाते होंगे) उसका प्रवेश द्वार मानो
सोने के बर्तन से ढका हुआ है (तेजोदीप्त हिरण्मय पुरुष के बारे में ऐसी बात कही जा
रही होगी; इसका आशय उस दीप्ति से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए जिसका आश्रय होनेसे दूरी
को तेजोमय दीप्ति और आभा मिल पाई)। हे सूर्य देवता इस आवरण को हटा दें ताकि मैं जो सत्य की पूजा करता रहा हूँ, उसे
महसूस कर सकूं; उसके स्वरुप पर ध्यानस्थ हो सकूं; सत्याश्रयी होकर जगदीश्वर के उस रूप
को भी अनुभव कर सकूं; जिसके आश्रय होने से हिरण्मय पुरुष और विज्ञानमय पुरुष कार्य
- ब्रह्म रूप में व्याप्त रहते हैं; प्रकृति के अवयवों को चैतन्यमय बनाते हैं ।
पुष्पानेकर्षे यम सूर्य
प्रजापत्य व्यूह रश्मिन्समुहा |
तेजः यत्ते रूपं कल्याणात्मं
तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि || ईशावास्योपनिषद श्लोक १६ ||
हे सूर्य देव, (स्वर्ग
के एकमात्र यात्री, सबके नियंत्रक, प्रजापति के पुत्र) , अपनी किरणों को हटाते हुए
छटाओं को समेत लें ताकि मैं (जो आपके भीतर के हिरण्मय पुरुष की भाँति एक विज्ञानमय
पुरुष हूँ ) आपके गौरवशाली रूप को देख सकूं।
वायुरानिलामृतमथेदं
भस्मान्तं शरीरम् |
ॐ | क्रतो स्मर कृतं
स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर || १७ ||
"(मेरा) प्राण
सर्वव्यापी वायु में, सनातन सूत्रात्मा में विलीन हो जाए ; स्थूल शरीर अग्नि द्वारा
भस्म हो जाए; मन को इस सत्य और अवश्य परिणाम का स्मरण करना होगा; बार बार स्मरण करना
होगा; विनाशी शरीर और अविनाशी विज्ञानमय पुरुष के बीच के भेद का भी परिचायक एक सत्य
है; जिसके आधार पर भौतिक शरीर को भी हिरण्मय पुरुष के अनुकम्पा से प्रकृति में विलीन होना होगा।
अग्ने नय सुपथा राये
अस्मान्विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् |
युयोध्यास्मज्जुहुराणामेनो
भूयिष्ठां ते नाम उक्तिं विधेम || १८ ||
"अग्नि से यह वंदना
की जा रही है कि साधक को कर्मों के फल भोगने के लिए अच्छे मार्ग पर ले चलें और मन से
चल काट के पा को दूर कर दें। "