[श्रीमद्भागवद्गीता और भागवत पुराण
के आलोक में शत्रु मित्र विषयक विवेक कि विवेचना]
चन्दन सुकुमार सेनगुप्ता
हम कभी कभी
इस भ्रम में पड़ जाते कि
कोई व्यक्ति हमारा शत्रु बनकर हमारे सामने संदर्भित हुआ या फिर मित्र
बनकर आया! यह निर्णय कर
पाना कभी कभी काफी कठिन भी हो जाता
कि हम शत्रु कि
तलाश सिर्फ बाहरी दुनिया में ही करते रहें
या फिर कभी कभी अंतर मन में भी
झांककर देखें? प्रश्न यह भी निर्माण
हो जाता है कि शत्रु
कि पहचान अगर करने लगें और सिर्फ पहचान
कर पाने तक ही सीमांकित
रहें तो क्या उस
गतिविधि से कोई निर्णायक
स्थिति तक हम पहुँच
भी पाएंगे ? हम इस बात
से भी कभी कभी
किनारा कर लेते हैं
कि शत्रु भाव से उत्पन्न ज्ञान
और विधायक कर्म को शायद ही
पूरी तरह प्रशमित किया जा सके।
शत्रु मित्र भाव को ठीक से
समझने के लिए हमें
शास्त्र सम्मत व्याख्यान और सूत्रों का
सहारा लेना होगा। वेद,
वेदांत, पुराण , आगम आदि विविध श्रोत से अंततः हम
यही पाते हैं कि शत्रु - मित्र का भाव एक मानसिक
स्थिति है जिस आधार पर व्यक्ति कर्म और जीवन चर्या के बारे में निर्णय ले लिया करता
है और उसी आधार पर खुद को कर्म तत्परता से भी जोड़ लिया करेगा। यहाँ व्यक्ति के अंदर निहित दोष गुणका भी आधार लेना
होगा ; कारण यह मान लिया जाएगा कि प्रकृति के अधीन होने के कारण व्यक्ति में दोष और
गुण दोनों ही रहेंगे; इस विधान से परे कोई साधक अगर खुद के आचरण में शुद्धता लाते हुए
निखरता चलेगा तो जाहिर सी बात है कि उनमें दोष घटता चलेगा और गुणों का संवर्धन होता
चलेगा।
गीता के अनुसार भी हम यह सत्यापित कर
पाएंगे कि “अपने द्वारा
अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे; क्योंकि
आप ही अपना मित्र
है और आप ही
अपना शत्रु है।“[1] अपने
स्वरूपसे जो एकदेशीय 'मैं-
पन दिखता है। उससे भी अपने को
ऊँचा उठाये।[2]
कारण कि शरीर इंद्रियाँ
आदि और ‘मैं[3]’-
पन- ये
सभी प्रकृति के कार्य हैं;[4]
अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप
नहीं है, उससे अपने को ऊँचा उठाये।
अगर यह अपना उद्धार करने में, अपने को ऊँचा उठाने
में शरीर, इंद्रियाँ, मन, बुद्धि आदि की सहायता मानेगा,
इनका सहारा लेगा तो फिर जड़ता
का त्याग कैसे होगा? क्योंकि जो अपने हैं,
अपने में है, अभी है और यहाँ
हैं, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के
लिए शरीर, इंद्रियाँ, मन, बुद्धि की आवश्यकता नहीं
है।[5]
कारण कि असत के
द्वारा सत की प्राप्ति
नहीं होती, प्रत्युत असत के त्याग से
सत की प्राप्ति होती
है।[6] इस क्रम में बने चरित का कर्मयोग[7] का
आश्रय लेना भी काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा।
योग , सांख्य और वेदांत का
कुशल समन्वय होने के बाद भी
अगर हम यह महसूस
करने लग जाएँ कि
शत्रु और मित्र का
भाव और किसीको इस
भाँती समझ पाने कि भावना अगर
हमारे मन में पनपती
हो तो यह मान
लेना होगा कि शुद्ध रूप
से हमारे अंदर ज्ञान और चेतना का
संचार नहीं हो पाया। अगर चेतना का संचार सही
स्वरुप में हुआ होता तो शायद ही
व्यक्ति अपने मन में किसी
के प्रति शत्रु भाव को पनपने दे
और शायद ही शत्रु भाव
के आवेश में आकर कुछ विपरीत आग्रह से किसी गतिविधियों
को अनजाम देने के निमित्त से
अग्रसर हो।
यह भी सर्वजन
विदित सत्य ही मानकर चलें
कि हम शायद ही
यह पता कर पाते हों
कि हमारे भीतर शत्रु भाव पनपने देने के लिए, किसी
ख़ास विषय से मुंह मोड़
लेने के लिए, किसी
दुराग्रह में आकर रचनाधर्मिता के विपरीत कुछ
कर गुजरने के लिए सूचक
तत्व कैसे पनपते होंगे ; यहाँ तक कि उस
आवेश से निकल पाने
के लिए हम किस प्रकार
से प्रयास करें जिससे हमारे भीतर पनपने वाले उन विपरीत धर्मी
गुणों को हटाया जा
सके और कुछ रचनाधर्मिता
को संवर्धित करने लायक गुणों को विकसित किया
जा सके। इस
क्रम में ज्ञान योग और भक्ति योग[8]
का सही सम्मलेन होना भी बहुत ही
आवश्यक और विधायक तत्व
माना जा सकेगा। [9]
इस दृष्टि से
मनुष्य अपनी विचार शक्ति को काम में
लेकर किसी भी योग मार्ग
से अपना कल्याण कर सकता है।
विचार करना चाहिए कि जितने दिन
रखना चाहूँ, उतने दिन नहीं रह सकता और
जैसा सबल बनाना चाहूँ, वैसा बन नहीं सकता।
यह शरीर ‘मेरे लिए’ भी नहीं है;
क्योंकि यदि यह मेरे लिए
होता तो इसके मिलने
पर मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। दूसरी बात, यह परिवर्तनशील है
और मैं अपरिवर्तनशील हूँ। परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील के काम कैसे
आ सकता है? नहीं आ सकता। तीसरी
बात, यदि यह मेरे लिए
होता तो सदा मेरे
पास रहता। परंतु यह मेरे पास
नहीं रहता। इस प्रकार शरीर
मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए
नहीं- इस वास्तविकता पर
मनुष्य दृढ़ रहे, तो अपने आपसे
अपना उद्धार हो जाएगा।
जागरूकता के कई पैमाने हो सकते हैं
पर सबसे बड़ा पैमाना आत्मिक और बौद्धिक स्थिरता
से ही समझी जा सकेगी ।[10] उस
स्थिरता का ही नतीजा है कि भक्त अपने निकट भगवान कि सन्निधि महसूस कर पाता है और उसी
के अनुसार उसके चरित्र कि दृढ़ता का भी निर्माण हो जाया करता है। उद्धार हो जाने का प्रश्न खुद के प्रयत्न से ही हो
जाय करेगा ; माता अहल्या उस रस्ते पर शिला बनकर पड़ी रही और श्री रघुनायक के आने का
इंतज़ार करने लगी; उमा और भवानी खुद को महादेव के पास समर्पित करके यह उम्मीद रखने लगी
कि उन्हें सर्वशक्तिमान जगदीश्वर स्वीकार कर लें ; कुछ ऐसी ही तपस्या के बारे में कन्याकुमारी
विषयक व्याख्यानमाला प्रचलित हुआ और साधक के लिए मिसाल कायम कर दिया गया। जब आचार्य श्री शंकर से उनका परिचय पुछा गया तो
उन्होंने अपने अंतर मन में सर्वशक्तिमान महादेव के अधिस्थान का विषय बताने लगे। अगर हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार हो जाएँ,
परम सत्ता के सम्मुख हो जाएं तो मनुष्य जन्म जैसी परिस्थिति और कलियुग जैसा मौका होते हुए भी कई बार खुद का
उद्धार कर पाने में समर्थ हो सकेंगे।
योगी को हम कभी कभी युक्त[11] कह
सकेंगे ; वह ख़ास परिस्थिति बनती होगी जब हम ऐसा कर पाते होंगे।
ज्ञान और भक्ति का सही सम्मलेन ही वह
पड़ाव है जहाँ से कर्म को एक सही दिशा मिल जाया करेगी और व्यक्ति अपने लिए एक निर्णायक
मार्ग कि तलाशी कर सकेगा ; उसे अंतरात्मा के साथ जुड़े हुए परमात्मा का सान्निध्य भी
अनुभव होता रहेगा।
------------
भगवान, संत महात्मा आदि के रहते हुए
हमारा उद्धार नहीं हुआ है कि इसमें
उद्धार की सामग्री की
कमी नहीं रही है अथवा हम
अपना उद्धार करने में असमर्थ नहीं हुए हैं। हम अपना उद्धार
करने के लिए तैयार
नहीं हुए, इसी से वे सब
मिलकर भी हमारा उद्धार
करने में समर्थ नहीं हुए। पर यह तब
होगा, जब हम स्वयं
अपना उद्धार करना चाहेंगे।
दूसरी बात, स्वयं ने ही अपना
पतन किया है अर्थात इसने
ही संसार के संबंध को
पकड़ा है, संसार ने इसको नहीं
पकड़ा है। जैसे, बाल्यावस्था को इसने छोड़ा
नहीं, प्रत्युत वह स्वाभाविक ही
छुट गयी। फिर इसने जवानी के संबंध को
पकड़ लिया कि ‘मैं जवान हूँ’, पर इसका जवानी
के साथ भी संबंध नहीं
रहेगा। तात्पर्य यह हुआ कि
अगर यह नया संबंध
नहीं जोड़े तो पुराना संबंध
स्वाभाविक ही छूट जाएगा,
जो कि स्वतः छूट
ही रहा है। पुराना संबंध तो रहता नहीं
और नया संबंध यह जोड़ लेता
है- इससे सिद्ध होता है कि संबंध
जोड़ने और छोड़ने में
यह स्वतंत्र और समर्थ है।
अगर यह नया संबंध
न जोड़े, तो अपना उद्धार
आप ही कर सकता
है। शरीर संसार के साथ जो
संयोग (संबंध) है, उसका प्रतिक्षण स्वतः वियोग हो रहा है।
उस स्वतः होते हुए वियोग को संयोग अवस्था
में ही स्वीकार कर
ले तो यह अपने
आपसे अपना उद्धार कर सकता है।
‘स्वयं
चेतन और एकरूप रहते
हुए भी इन प्राकृत
चीजों के पराधीन हो
जाता है और अपना
पतन कर लेता है।[12]
बड़े आश्चर्य की बात है
कि इस पतन में
भी यह अपना उत्थान
मानता है और उनके
अधीन होकर भी अपने को
स्वाधीन मानता है।
तात्पर्य
है कि प्राकृत पदार्थ
इसके साधक (सहायक) अथवा बाधक नहीं है। यह स्वयं ही
अपना उद्धार कर सकता है,
इसलिए यह स्वयं ही
अपना बंधु (मित्र) है। हमारे जो सहायक हैं,
रक्षक हैं, उद्धारक हैं, उनमें भी जब हम
श्रद्धा- भक्ति करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तभी वे हमारे बंधु
होंगे, सहायक आदि होंगे। अतः मूल में हम ही हमारे
बंधु हैं; क्योंकि हमारे माने बिना, हमारे श्रद्धा विश्वास किए बिना वे हमारा उद्धार
नही कर सकते- यह
नियम है।
अपने सिवाय इसका कोई दूसरा शत्रु नहीं
है।[13] प्रकृति
के कार्य शरीर, इंद्रियाँ, मन, बुद्धि आदि भी इसका अपकार करने में समर्थ नहीं है। ये
शरीर, इंद्रियाँ आदि जैसे इसका अपकार नहीं कर सकते, ऐसे ही इसका अपकार नहीं कर सकते.
ऐसे ही इसका उपकार भी नहीं कर सकते। जब स्वयं उन शरीरादि को अपना मान लेता है, तो यह
स्वयं ही अपना शत्रु बन जाता है। तात्पर्य है कि उन प्राकृत पदार्थों से अपने पन की
स्वीकृति ही अपने साथ अपनी शत्रुता है।
जिस जीवात्मा द्वारा स्वयं (मन) को जीता हुआ
है, वह जीवात्मा स्वयं
का मित्र है और जिसके
द्वारा अपना मन नहीं जीता
गया है, उसके लिए वह शत्रु के
सदृश ही आचरण करता
है॥6॥[14]
[1] उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ।। 6.5 ।।
[2] '‘उद्धरेदात्मनात्मानम्’- अपने आपसे अपना उद्धार करे- इसका तात्पर्य है कि शरीर,
इंद्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपने आपको
ऊँचा उठाए।
[3] अपना स्वरूप परमात्मा के साथ एक
है और शरीर, इंद्रियाँ
आदि तथा ‘मैं’- पन प्रकृति के
साथ एक है।
[4] ‘मैं’ शरीर नहीं हूँ; क्योंकि शरीर बदलता रहता है और मैं
वही रहता हूँ। यह शरीर ‘मेरा’
भी नहीं है; क्योंकि शरीर पर मेरा वश
नहीं चलता अर्थात शरीर को मैं जैसा
रखना चाहूँ, वह वैसा नहीं
कर सकता;
[5] प्राकृत पदार्थ, क्रिया और संकल्प में
आसक्त न हो, उनमें
फँसे नहीं, प्रत्युत उनसे अपने आपको ऊपर उठाये। यह सबका प्रत्यक्ष
अनुभव है कि पदार्थ,
क्रिया और संकल्प का
आरंभ तथा अंत होता है, उनका संयोग तथा वियोग होता है, पर अपने (स्वयं
के) अभाव का और परिवर्तन
का अनुभव किसी को नहीं होता।
जड़ वस्तुओं से संबंद्ध मानना, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना ही खास बंधन है।
[6] उत्पन्न और नष्ट होने
वाले पदार्थ आदि में न फँसना उनके
अधीन न होना, उनसे
निर्लिप्त रहना ही अपना उद्धार
करना है। मनुष्य मात्र में एक ऐसी विचार
शक्ति है, जिसको काम में लाने से वह अपना
उद्धार कर सकता है।
[7] ‘कर्मयोग’
का साधक उसी विचार शक्ति से मिले हुए
शरीर, इंद्रियाँ, मन, बुद्धि आदि पदार्थों को संसार का
ही मानते हुए संसार की सेवा में
लगाकार उन पदार्थों से
संबंध विच्छेद कर लेता है
और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।
[8] ‘भक्तियोग’ का साधक उसी
विचार शक्ति से ‘मैं भगवान का हूँ और
भगवान मेरे हैं’ इस प्रकार भगवान
से आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है।
[9] ‘ज्ञानयोग’
का साधक उस विचार शक्ति
से जड़ चेतना का अलगाव करके
चेतन (अपने स्वरूप) में स्थित हो जाता है
और जड़ (शरीर-संसार) से संबंध विच्छेद
कर लेता है।
[10] जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः।
शीतोष्णसुखदुःखेषु
तथा मानापमानयोः॥६-७॥
“सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख और मान-अपमान
में जिसने स्वयं को अविचलित रख
पा रहा होगा और जिसे ध्येय
मार्ग से किसी भी
परिस्थिति में अलग न किया जाता
हगा उस जीवन का
संचरण सदैव ही परमात्मा
में सभी प्रकार
से प्रतिस्थापित हो चूका होगा
ऐसा मानकर ही चलना चाहिए।“
[11] ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः।
युक्त
इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः॥ गीता अध्याय ६- श्लोक ८॥
जो
(औपनिषदिक) और दिव्य ज्ञान,
(आत्म अनुभव रूपी और बौद्धिक उत्कर्ष
दिलाने लायक) विज्ञान से तृप्त है,
विकाररहित है, इन्द्रियों को नियंत्रण में
ला चूका और
जिसके लिए सभी वास्तु एक समान हो
गए होंगे, ऐसे योगी को हम युक्त
कह सकेंगे।
[12] ‘आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः’- यह आप ही
अपना बंधु है। अपने सिवाय और कोई बंधु
है ही नहीं। अतः
स्वयं को किसी की
जरूरत नहीं है, इसको अपने उद्धार के लिए किसी
योग्यता की जरूरत नहीं
है, शरीर, इंद्रियाँ, मन, बुद्धि आदि की जरूरत नहीं
है।
[13] ‘आत्मैव रिपुरात्मनः’- यह आप ही
अपना शत्रु है अर्थात जो
अपने द्वारा अपने आप का उद्धार
नहीं करता, वह अपने आप
का शत्रु है। अपना मित्र और शत्रु आप ही है,
दूसरा कोई मित्र और शत्रु हो ही नहीं सकता और होना संभव भी नहीं है। नात्मानमवसादयेत’-
यह अपने आपको पतन की तरफ न ले जाए- इसका तात्पर्य है कि परिवर्तनशील प्राकृत पदार्थों
के साथ अपना संबंध न जोड़ें अर्थात उनको महत्त्व देकर उनका दास न बने, अपने को उनके
अधीन न माने, अपने लिए उनकी आवश्यकता न समझे। जैसे किसी को धन मिला, पद मिला, अधिकार
मिला, तो उनके मिलने से यह अपने को बड़ा, श्रेष्ठ और स्वतंत्र मानता है, पर विचार करके
देखें कि यह स्वयं बड़ा हुआ कि धन, पद, अधिकार बड़े हुए? प्रकृति के कार्य के साथ किञ्चिन्मात्र
भी संबंध मानने से यह आप ही अपना शत्रु है।
[14] बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्॥६-६॥
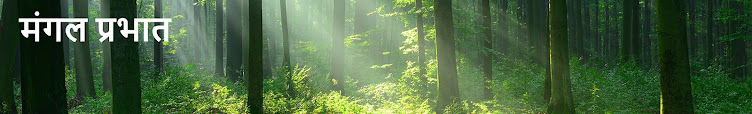






.jpg)
