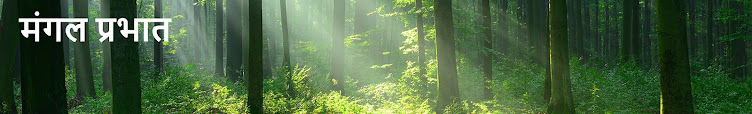भक्ति
मार्ग काफी सरल भी है और काफी जटिल भी; यह निर्भर करता होग्गा उस भक्त के स्वरुप के
ऊपर जिसे अपने रूचि के अनुसार कर्म, भक्ति या ज्ञान की धारा का अवलम्बन लेते हुए जगदीश्वर
के सन्निकट खुद के अस्तित्व का अनुसंधान करना है; खुद की भूमिका बांधना है, और दिव्य
जन्म को सार्थक करते हुए दिव्य कर्म के लिए प्रवृत्त होना है। [i] 'मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ताः उपासते' --
मन वहीं लगता है, जहाँ प्रेम होता है। जिसमें प्रेम होता है, उसका चिन्तन स्वतः होता
है; "नित्ययुक्ताः " का टाटरी हुआ सदा सर्वदा हर परिस्थिति में आत्मा के
समीप जगत के नियंता परम तत्व के रूप में जगदीश्वर के अधिष्ठान का अनुभव करते हुए नित्य
क्रिया (यज्ञ, दानं और तप ) में लगे रहना; क्रमशः उस गहराई तक खुद को ले जाना जहां
आत्मा और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता होगा; जहां से सिर्फ पूर्णता पाने का मार्ग
शेष रहता होगा; जहां के बाद हम जगदीश्वर के पास शरणागति पाकर अभय रूप धन के धनी बन
जाते होंगे; जिसके बाद कुछ भी पाने लायक शेष नहीं रह जाता; जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ
जगदीश्वर के अधिष्ठान विषययक सत्य की ही अनुभूति शेष रहती होगी। हर परिस्थिति में यह
कहना भी समीचीन न होगा कि मन की वृत्तियाँ आराम से साधक के नियंत्रण में आ जाए और उसे
भक्तिमार्ग का पथिक बना दे, अनन्य भक्ति की धारा में लगा दे और वैसा अभ्यास करने के
लिए सुगमता से लगा दे जिसके बाद जगदीश्वर को साधक अपने ही सन्निकट अधिष्ठान होता हुआ
महसूस करने लग जाए। इस दृष्टि से भी साधना में “निरंतरता” का महत्व माना गया; भक्त
को प्रयत्न करते ही रहना होगा; भक्ति की धारा में भक्त को क्रमशः आगे ही चलना होगा
; किसी भी पड़ाव की चिंता छोड़कर क्रमिक उन्नति और क्रमिक परिपक्वता की ओर।
श्रीमद्भागवद्गीता
में अनन्य भक्त के लालक्षणों को स्थान स्थान पर कई प्रकार से संदर्भित किया गया; उस
सन्दर्भ की पुष्टि के लिए कई व्याख्यान भी रचे गए; अंततः भक्त को ही जगदीश्वर के व्याप्ति
की अनुभूति हो सकेगी इस आशा की पुष्टि की गई।[i]
[i]
अनन्य भक्तके लक्षणोंमें तीन
विध्यात्मक '(मत्कर्मकृत्, मत्परमः और मद्भक्तः)' और दो निषेधात्मक '(सङ्गवर्जितः'
और 'निर्वैरः') पद का उल्लेख हुआ : (अध्याय ११, श्लोक ५५ ): 'सर्वाणि
कर्माणि मयि संन्यस्य' पदोंसे 'मत्कर्मकृत्' की बात कही गई; 'मत्पराः' पदसे 'मत्परमः'
का संकेत; 'अनन्येनैव योगेन' पदोंमें 'मद्भक्तः' के बारे में ऐसी बात कही गई; जगदीश्वर
में ही अनन्यतापूर्वक लगे रहनेके कारण उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती अतः वे 'सङ्गवर्जितः'
माने गए। कहीं भी आसक्ति न रहनेके कारण उनके
मनमें किसीके प्रति भी वैर ("अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः
" -- इस सूत्र के जरिये भी महर्षि पतंजलि वैर त्याग के महत्व को बताते आये ),
द्वेष, क्रोध, विषाद आदिका भाव नहीं रह जाता;
'निर्वैरः' पदका भाव भी इसीके अन्तर्गत मानी गई ; 'अद्वेष्टा' पदका प्रयोग (अध्याय
१२, श्लोक १३ ) इसी दृष्टि से किया गया; साधकको किसीमें सामान्य मात्रा में भी द्वेष
और ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए ( सर्वं खल्विदं ब्रह्म " महावाक्य के जरिये उसी आशय
की पुष्टि हो सकी); 'मयि संन्यस्य' पदोंसे जगदीश्वर का उद्देश्य क्रियाओंका स्वरूपसे
त्याग करनेका नहीं है। स्वरूपसे कर्मोंका त्याग सम्भव नहीं (गीता अध्याय ३ । श्लोक
5 । अध्याय १८ । श्लोक ११ )। सगुन उपासना में
भी कर्म का त्याग अगर किया ही जाता है to यह त्याग तामस होगा (गीता अध्याय १८ । श्लोक
७ )। शारीरिक क्लेश के भय से कर्म का त्याग राजस होगा (अध्याय १८ , श्लोक ८ )
[i]
"एक नौका के द्वारा किसी
सड़क मार्ग की यात्रा नहीं की जा सकती ; न हवाई
जहाज के द्वारा समुद्र यात्रा; न ही साइकिल
से साठ मील प्रति घंटे की गति से दूरी तय किया
जा सकता; प्रत्येक वाहन की अपनी सीमाएं, विशेषताएं और उपयोगिताएं हैं। परन्तु किसी भी साधन का बुद्धिमत्ता तथा कौशल
का सावधानीपूर्वक उपयोग करने से गन्तव्य तक पहुँचा जा सकता है; सही प्रकार के वाहन
को उपयोग में भी लाया जा सकता है। आत्मविकास
के लिए, खुद को जगदीश्वर के समीप उपलब्ध पाने के लिए [ जो कि एक चिरंतन सत्य, सर्व
जान विदित भवितव्य और न टालनेयोग्य सम्मलेन स्वरुप माना गया; जिसे साधक कुछ प्रयत्न
मात्र से ही अनुभव करने लग जाते होंगे; जिसे एक प्राप्त की ही प्राप्ति मानी गई; जिसे
पाने अर्थ हुआ नदी की धारा का समुद्र के विस्तीर्ण जालजलराशि में जाकर विलीन हो जाना;
जिसे पूर्णता पाने के क्रम में बढ़ाया जानेवाला वलिष्ठ कदम भी माना जाएगा ]; प्रत्येक
साधक उपलब्ध शरीर, मन और बुद्धि की उपाधियों में से किसी एक की प्रधानता से कर्मयोग,
भक्तियोग या ज्ञानयोग के मार्ग का चुनाव करता होगा ; जैसे त्रिवेणी की धारा में से
तीनों धारा को अलग से छांट पाना कठिन हो जाता होगा वैसे ही योग के तीन प्रमुख धारा
में से तीनों का सूक्षमता पूर्वक अनुसरण कर पाना भी कठिन हो जाता है; वस्तुतः इन धाराओं
को अलग कर भी नहीं पाएंगे; किसी एक धारा की प्रधानता जरूर रहती होगी; इसी दृष्टि से
हम ज्ञान योगी, उत्तम भक्त या ज्ञानी साधक को विशेषित कर पाते होंगे। प्रकृतिसे जीव
का माना हुआ सम्बन्ध विषयक भ्रम दूर होते ही जगदीश्वर से अपना वास्तविक और नित्यसिद्ध सम्बन्ध प्रकट होने
लग जाता है ; उसकी स्मृति से अपना स्मृति पटल भी आप्लुत होने लग जाएगा -- 'नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा' (गीता अध्याय १८
। ७३ )। 'ते मे युक्ततमा मताः (अध्याय १२ श्लोक २)' बहुवचनान्त पदसे जिस विषय का प्रतिआदान
हुआ , यही बात 'स मे युक्ततमो मतः (अध्याय
६, श्लोक ४७ )' एकवचनान्त पदसे पहले कही जा चुकी। “
[श्रीमद्भागवद्गीता,
अध्याय १२, श्लोक २- ५ का आधार ]
----
आदि गुरु शंकराचार्य, योगी रामसुखदास, स्वामी गम्भीरानन्द जी, स्वामी तेजोमयानन्दजी,
स्वामी रामभद्राचार्य जी आदि भाष्यकारों और टीकाकारों के सम्मिलित विवेचना के आधार
पर।।