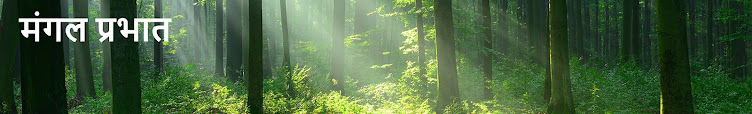सृष्टि रचना में योगमाया का ही इस्तेमाल ईश्वर किया करते हैं; उसी योगमाया के कारण हम दृश्य जगत में निहित परम सत्ता को प्रत्यक्ष रूपप से किसी इन्द्रियग्राह्य अवयव के रूप में नहीं देख पाते; और कभी कभी ईश्वर उसी योगमाया के कारण हमारे सम्मुख एक क्रियाशील माया रचना के रूप में रकत होकर हमें भी उस और प्रवृत्त हो जाने के लिए प्रबुद्ध करते रहते है। .
अप्रत्यक्ष रूप से यही अविद्या माया है, जिसके आवेश में आकर साधक महात्मा भी कभी कभी भ्रमित हो जाते और ईश्वर के जरिये भगवान के वितरित होते रहने के रहस्य को भली भाँति नहीं जान पाते। पुरुष का कर्म ज्ञान कृत होने के कारण प्रकृति के जरिये अभिव्यक्त होते समय एक स्वच्छंदत और निरलस भाव को बनाये रखते हैं और उसी निर्मलता से ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय संकुल के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए मन, स्मृति और बुद्धि को कर्म में प्रवृत्त करते रहते हैं; वहीँ से कर्तव्य निर्धारण में भी उनकी ही एकमेव भूमिका बनती है; सृष्टि चक्र में व्याप्प्त इस निम्नवर्ती अभिव्यक्ति के चक्र से उन्नत होने के निमित्त से साधना में भी लगने के लिए उद्योगी होते हैं; साधना के मार्ग का चयन बुद्धि और कौशल्य के आधार पर कर लिया करते हैं; एक उन्नत पैमाने पर अन्य जीव के लिए प्रेरणा का श्रोत भी बन जाते हैं। जड़ शरीर में प्राण संचार के बाद ही विधायक पुरुष का कर्म में प्रवृत्त होना ही एक सहजात नियति है, जिसके अधीन जीव को जन्म और मृत्यु के बीच फैले संचार पथ से होकर कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होते हुए ही अग्रसर होना होगा; उन्नत जीवनशैली के लिए प्रत्नशील होना होगा; दिव्य ज्ञान से खुद को पुष्ट करना होगा; विवर्तन की धारा में चलते हुए देवत्व के आसान को अलंकृत करने के लिए दिव्य कर्म का अनुष्ठान भी करना होगा; उस मार्ग में आनेवाली बाधाओं को झेलना होगा; परम पुरुष के परम सत्ता को समझते हुए वैसी ही पूर्णता पाने के लिए भी अनुरक्त होना होगा।
जगदीश्वर होते ही हैं सर्व कल्याण कारण ; सर्व नीति नियंता और सर्वभूते निहित आत्मा। उन्हें अनुभव करने का और आत्मा के साथ एकरूपता की स्थिति में महसूस कर पाने का ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म को माना गया। एक बार ब्रह्मा निर्वाण की अवस्था पाने के बाद व्यक्ति कभी भी मोह के वशीभूत नहीं होता
। अनावश्यक रूप से कर्म बंधन में जकड़े जाने से माया से व्याप्त दृश्य जगत के रंग बिरंगे
व्यवधान आदि में मन को न लगाते हुए उस परमेश्वर
के अंशमात्र को खुद के चेतन स्वरूप में टटोलना होगा; वहां से मिलनेवाले दिव्य निर्देश
को मान्य करते हुए अनन्य भाव से उसी ईष्ट की आराधना में भी लगाना होगा। भगवद्प्राप्ति
के बाद भक्त में कुछ विशेष परिवर्तन आना अवश्यम्भावी है: परा भक्ति के द्वारा ईश्वर
को (परम ब्रम्ह स्वरुप को) वह तत्त्वत: जानता है कि मैं वह परमेश्वर कितना व्यापक और
कितना फैला हुआ है; तथा ईष्ट क्या है।[1] इस प्रकार
तत्त्वत: जानने के बाद वैसा तत्ववेत्ता भक्त भगवत स्वरुप ही बन जाता है।
[1] भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः।
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्।।गीता १८ .५५ ।।
सा इयं ज्ञाननिष्ठा आर्तादिभक्तित्रयापेक्षया परा चतुर्थी भक्तिरिति उक्ता। तया परया भक्त्या भगवन्तं तत्त्वतः अभिजानाति? यदनन्तरमेव ईश्वरक्षेत्रज्ञभेदबुद्धिः अशेषतः निवर्तते। अतः ज्ञाननिष्ठालक्षणतया भक्त्या माम् अभिजानातीति वचनं न विरुध्यते। अत्र च सर्वं निवृत्तिविधायि शास्त्रं वेदान्तेतिहासपुराणस्मृतिलक्षणं न्यायप्रसिद्धम् अर्थवत् भवति -- विदित्वा৷৷৷৷ व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति (बृह0 उ0 3।5।1) तस्मान्न्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहुः (ना0 उ0
2।79)
न्यास एवात्यरेचयत् (ना0 उ0
2।78)
इति। संन्यासः कर्मणां न्यासः वेदानिमं च लोकममुं च परित्यज्य
(आप0
ध0
1।23।13) त्यज धर्ममधर्मं च ( महा0
शा0
329।40)
इत्यादि। इह च प्रदर्शितानि वाक्यानि। न च तेषां वाक्यानाम् आनर्थक्यं युक्तम् न च अर्थवादत्वम् स्वप्रकरणस्थत्वात्? प्रत्यगात्माविक्रियस्वरूपनिष्ठत्वाच्च मोक्षस्य। न हि पूर्वसमुद्रं जिगिमिषोः प्रातिलोम्येन प्रत्यक्समुद्रजिगमिषुणा समानमार्गत्वं संभवति।