["चन्दन सुकुमार सेनगुप्ता विरचित हे राम शीर्षक पुस्तक से "]
विधाता हमें कर्म में लगाकर सृष्टि में
निरंतरता लाने का प्रयास करते रहते हैं और एक क्रम से हमें भी उन्नति के मार्ग पर
बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं।
प्रकृति के गुणों के अधीन ही जीव कर्म के लिए प्रवृत्त होते हैं और विधायक
कर्म में लिप्त होते रहते हैं। [i] वस्तुतः एक क्षण के लिए भी व्यक्ति पूर्ण
निष्क्रियता से नहीं रह सकता; यदि सिर्फ बैठे हों तब भी कुछ न कुछ तरंगों से मन
अशांत हुआ रहता होगा; गहन निद्रा में भी हम स्वप्नलोक में सक्रिय रहते होंगे। निद्रा में भी श्वास और संवहन की क्रिया के साथ
साथ स्वयःक्रिय स्नायु की क्रिया भी चला करेगी। अतः यह भी कहा जा सकेगा कि पूर्ण
समाधि जैसी स्थिति में भी हम सक्रिय रहते होंगे और विश्व चराचर के इस पार्थिव जगत
में चेतना सहित वापस आने के लिए प्रयत्न कर लिया करेंगे ; अगर सफलता मिली तो
सक्रिय हुए और विफलता मिली तो शरीर छूटा! बीच के अंर्तवर्ती पर्याय में ही चेतना
का आवागमन होता रहेगा।
श्रेष्ठ वही कहलायेंगे जो ज्ञानेन्द्रिय को वश में करके
कर्मेन्द्रियों को आसक्ति रहित होकर
विधायक कर्म में लगा सकेंगे। [ii] प्रजा पालन और प्रजा रक्षण के बारे में कहा
जाता है: ब्रह्मा प्रजापालक हैं और प्रजा के कल्याण के लिए भी तत्पर रहते हैं। [iii]
पूर्ण कर्मयोगी तो सभी कर्म यज्ञ के रूप
में ही किया करेंगे; [iv] भोजन
करते समय भी जठराग्नि रुपी कुंड में भोजन रुपी द्रव्य कि आहूति देंगे। संग्रह
वृत्ति से बचते हुए कर्मयोगी को विधायक कर्म में लगाना चाहिए। [v]
[i] न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् । कार्यते
ह्यवश: कर्म सर्व: प्रकृतिजैर्गुणै: ।। श्रीमद्भागवद्गीता अध्याय ३ श्लोक ५ ।।
न – नहीं ; नमस्ते - अवश्य ; कश्चित् – कोई भी ;
क्षणम् – एक क्षण ; अपि – सम ; जातु – सदैव ; तिष्ठति – रह सकता है ; अकर्म-कृत - कर्म
के बिना ; कार्यते – किये जाते हैं ; नमस्ते - अवश्य ; अवशः – असहाय ; कर्म - कार्य
; सर्वः – सभी ; प्रकृति-जैः – भौतिक प्रकृति से उत्पन्न ; गुणैः – गुणों से
[ii] यस् त्विन्द्रियानि
मनसा नियम्यारभते 'अर्जुन
कर्मेन्द्रियैः कर्म-योगम् असक्तः स
विशिष्यते।। श्रीमद्भागवद्गीता अध्याय ३ श्लोक ७।।
यः – कौन ; तू - परंतु ; इन्द्रियाणि
– इन्द्रियाँ ; मनसा – मन से ; नियम्य – नियंत्रण ; अरभते - प्रारंभ होता है ; अर्जुन
– अर्जुन ; कर्म-इन्द्रियैः – कर्मेन्द्रियों द्वारा ; कर्म-योगम् - कर्मयोग ; असक्तः
– आसक्ति रहित ; सः – वे ; विशिष्यते - श्रेष्ठ हैं;
[iii] सहयज्ञाः
प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्टकामधुक् ।।
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः
। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।।
……………… श्रीमद्भागवद्गीता अध्याय ३ श्लोक
१०, ११ ।।
“प्रजापति ब्रह्माजी ने सृष्टि के आदिकाल
में कर्तव्य-कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना करके उनसे कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य
के द्वारा सब की वृद्धि करो और वह कर्तव्य-कर्म-रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन
की आवश्यकता सामग्री प्रदान करने वाला हो। अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं
को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस
प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे।“
[iv]
गृहेश्व अविशतम् चापि पुंसाम कुशल-कर्मणाम् मद-वर्त-यत-यमानं न बंधाय गृह मतः (भागवत
४-३०-१९ (६)
“पूर्ण कर्मयोगी , अपने नित्य क्रिया और कर्तव्यों को पूरा
करते हुए भी, ईष्ट को सभी गतिविधियों का भोक्ता जानकर, ईष्ट के लिए अपने सभी कार्य यज्ञ के रूप में करते हैं।
[v] स विश्वजितं अजहरे यज्ञं सर्वस्व दक्षिणम्
अदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचम इव (रघुवंश ४ - ८६ )[ श्लोक ५]
"रघु ने विश्वजीत यज्ञ इस सोच के साथ किया था कि जैसे
बादल पृथ्वी से पानी इकट्ठा करते हैं, अपने आनंद के लिए नहीं, बल्कि उसे वापस पृथ्वी
पर बरसाने के लिए, उसी तरह, एक राजा के रूप में उनके पास जो कुछ भी था, वह जनता से
कर के रूप में एकत्र किया गया था, अपनी ख़ुशी के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की ख़ुशी
के लिए। अतः उन सभी संग्रहों को प्रजा हितार्थ खर्च करके फिर से भिक्षा पात्र लेकर
योगक्षेम का इंतजाम करने के लिए निकल पड़े ।“
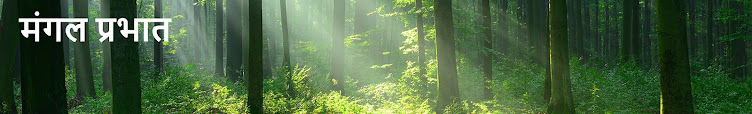







.jpg)